ऐसा क्या है कि सरकारी विद्यालय बनकर रह गए गरीब की पाठशाला, लेखक तलाश रहे इन प्रश्नों के उत्तर
आज के चकाचौंध दिखावे की धारा में सरकारी विद्यालय को गरीब की पाठशाला कहा जाता है आखिर ऐसा क्यों? इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए सरकारी स्कूल से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर नजर डाले तो कुछ समझा जा सकता है ऐसा क्या नहीं है इन सरकारी स्कूलों में जो निजी संस्थानों में है। जैसे इन सरकारी स्कूलों के भवन, शिक्षकों, शिक्षार्थियों एवं शिक्षण व्यवस्थाओं में जिनके कारण आज इनको गरीब की पाठशाला की उपाधि मिली है। एक सरकारी नौकर व्यवस्था के दृष्टिकोण से आकलन किया जाए तो सबसे अधिक भारतीय प्रशासनिक सेवा में, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में एवं राजपत्रित अधिकारियों का उत्पादन कर्ता एवं जननी सरकारी स्कूलों को ही माना जाता है। परंतु सरकारी नौकरों की भावनाओं की ओर दृष्टि डालकर के देखा जाए तो समझ में आता है कि सरकारी स्कूल गरीब की पाठशाला है। इसी कारण सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों का दाखिला शहर की नामी निजी संस्था में दिलवाता है। आखिर यह भेदभाव पूर्ण नीति नहीं है तो क्या है?
शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के सर्वे रिपोर्ट करवाई जाए तो संभव है कि 70 फीसद उनके बालकों का दाखिला निजी संस्थानों में मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों इस प्रश्न के प्रति क्या धारणाएं उनकी। अब प्रश्न यह है उठता है कि क्या है गरीब? सरकारी भवन, सरकारी मैदान, सरकारी विद्यालय में शिक्षण कराने वाले शिक्षक, सरकारी विद्यालय के शिक्षार्थी या फिर इन सभी की व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापक।
-सरकार द्वारा भवन निर्माण में लाखों, करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं फिर भी निर्मित भवनों में एक-दो वर्ष में वर्षा के मौसम में पानी टपकने से दयनीय स्थिति बन जाती है। कौन है जिम्मेदार इसका? जबकि उनके एक चौथाई रुपये में किसी निजी मकान या संस्था के भवन का अच्छा निर्माण होता है जो ताउम्र नष्ट नहीं होता है आखिर ऐसा क्यों?
-सरकार के द्वारा नियुक्त शिक्षकों को देखा जाए तो सातवें वेतनमान से उनको अच्छी पगार मिलने लगी है और अच्छा प्रशिक्षण देकर योग्य बनाया जा रहा है। वहीं, निजी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। उन सरकारी शिक्षक में से अधिकांश उच्च पदों पर अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। क्योंकि उसके अंदर योग्यताओं का अतुल्य भंडार हैं। आज राजस्थान के प्रशासनिक पदों में इन शिक्षकों की अहम् भूमिका नजर आती है। फिर ऐसे योग्य शिक्षकों को विद्यालय प्रांगण में हीन दृष्टि से क्यों देखा जाता है। वही शिक्षक तहसीलदार बनने पर सर्वे सर्वा समझा जाता है। यह विद्यालय के प्रति संकीर्ण विचारधारा नहीं है तो क्या है? ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आज शिक्षक स्वयं को असहाय कमजोर और गरीब समझता है क्या इसी कारण गरीब की पाठशाला है?
-सरकारी विद्यालय में शिक्षण करने वाला फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल, चिपका पेट वाला शिक्षार्थी गरीब है। उसको पोषाहार युक्त भोजन, वर्ष भर में मिलने वाली अनेक योजनाओं से जुड़ी छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। विद्यालय में शिक्षण हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान की जाती है। दूरी की अधिकता होने पर ट्रांस वाउचर या साइकिल व्यवस्था की जाती है। फिर भी क्यों शिक्षार्थी फटी पुरानी गणवेश, बिना बाल संवारे, फटे हाल जूते और अस्वच्छ होकर विद्यालय में प्रवेश करता है तो लगता है कि यह गरीब लोगों की पाठशाला है। दूसरी तरफ निजी संस्थानों में इन्हीं सभी सुविधाओं के अभाव के बावजूद भी एक अभिभावक शिक्षार्थी को सार संवार करके दिशा और दशा बदल लेता है आखिर ऐसा क्यों?
-सरकारी महकमे में विद्यालय स्तर से लेकर शिक्षा के उच्च पायदान के सर्वोच्च पदाधिकारी द्वारा निर्मित व्यवस्था को देखने पर कुछ समझ सकते हैं क्या यह व्यवस्था कमजोर हैं या व्यवस्थापक। किस कड़ी को दोष दे। दूसरी ओर निजी विद्यालयों में व्यवस्था ना होकर प्रबंधन कायम है कहीं इसी कारण तो नहीं।
आज देखें की व्यवस्था के कौन से स्तर पर कमजोरी हैं, जिसके कारण अव्यवस्था हो रही है। सरकारी तंत्र के द्वारा शिक्षण हेतु नवीन नवाचार होते हुए भी उसका पूरा लाभ शिक्षार्थियों को नहीं मिल रहा है। प्रत्येक स्तर की आपसी कड़ियों में संचार की कमी नजर आती है और पूरी व्यवस्था आंकड़ों में सीमित हो गई हैं। वास्तविकता के धरातल को जाने बिना कागजी आंकड़ों को ही लक्ष्य प्राप्ति का अंतिम द्योतक मान लिया जाता है। आज शिक्षा का सारा खेल विद्यालय मैदान में ना हो करके रैंकिंग और स्टार पर आधारित हो गया है। इसी कारण आज दीक्षा जैसे प्रशिक्षण भी केवल प्रमाण पत्र तक सीमित हो चुके हैं।
-अभिभावकों के विचारों में भी यह है कि सरकारी विद्यालय आज गरीब बच्चों के शिक्षण की पाठशाला है। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ जागरूक अभिभावक अपने बालक बालिकाओं का दाखिला श्रम ( मजदूरी) करके भी निजी शिक्षण संस्थाओं में करवाने की चाह रखता है चाहे फीस की भरपाई समय-समय पर क्यों ना हो?
ऐसे अनेक सवाल हैं जिनके कारण सरकारी स्कूल गरीबों की पाठशाला बनते जा रहे हैं कुछ प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं।कहीं इन कारणों से तो नहीं।
कारण:-
1-सरकारी भवनों की दुर्दशा (आकर्षक ना होना)।
2-विद्यालय प्रांगण में गार्डन (बगीचा) का ना ।
3-विद्यालय प्रांगण में खेल मैदान एवं खेल प्रतियोगिताओं का अभाव ।
4-शिक्षकों की शिक्षण के प्रति उदासीनता।
5शिक्षकों को शिक्षण में रोचक शिक्षण सामग्री का प्रयोग ना करना।
6-शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व कृतित्व को नकारना।
7-शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को प्रश्न उत्तर के लिए अवसर न देना।
8-शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों के हितैषी योजनाओं के प्रति उदासीनता।
9-विद्यालय के व्यवस्थापक के द्वारा व्यवस्थाओं को नजर अंदाज करना।
10-विद्यालय से अभिभावकों का बराबर ना जुड़ना (बैठकों को रजिस्टर तक सीमित रखना)
11-विद्यालय में पुस्तकालय को नकारा जाना।
12-ऑनलाइन के कच्चे धागों में विद्यार्थियों को बराबर नहीं जोड़ पाना ।
सुझाव:-
आज जिन क्षेत्रों में उपर्युक्त कारणों के साथ अन्य सुधारात्मक प्रयास हुए उन विद्यालयों को गरीब की पाठशाला न मानकर आदर्श पाठशाला माना जाने लगा है, परंतु अधिकांश विद्यालय में गुणात्मक सुधार का प्रयास अपेक्षित है।
1-उच्च माध्यमिक स्तर की विद्यालयों की मॉनिटरिंग व्यवस्था को प्रबंधन के साथ जोड़ा जाए।
2-विद्यालय प्रांगण में बगीचा जैसी हरित पाठशाला के तहत अनिवार्य हो।
3-खेल के प्रति जागरूकता अभियान में मासिक प्रतिपुष्टि अवलोकित हो ।
4-शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी के व्यक्तित्व विकास (पर्सनालिटी) पर विशेष जोर दिया जाए।
5-शिक्षण व्यवस्था को रोचक शिक्षण सामग्री के साथ वास्तविक परिवेश से जोड़ कर देखा जाए।
6-पुस्तकालय के प्रति शिक्षार्थियों का रुझान जागृत करने के लिए अवसर दिया जाए।
7-डिजिटल धागे को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर विशेष संयंत्रो के साथ जोर दिया जाए।
8-सरकारी योजनाओं से प्राप्त राशि का उपभोग बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास (वेशभूषा) पर जोर दिया जाए तथा यह कार्य प्रवेश के समय अनिवार्य हो।
9-व्यवस्थापक व्यवस्थाओं को नजरअंदाज ना करके भामाशाह सहयोग से प्रबंधन करने का प्रयास किया जाए।
10-विद्यालय के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण को बदलने के लिए उनको विद्यालय प्रांगण से जोड़ने का प्रयास हो। तथा बालकों को प्रगति रिपोर्ट से समय-समय पर अवगत कराया जाकर प्रोत्साहित करें।
11-हर पेशे से जुड़े व्यक्तित्व को विद्यालय से जोड़कर देखा जाए तथा उचित मार्गदर्शन दिया जाए जैसे IAS, IPS, IES RAS RTS, RJS, DOCTOR, ENGINEER, POLICE, SCIENTISTS आदि ।
12-अभिभावक की संकीर्ण विचारधारा में बदलाव।
13-इस बदलाव के लिए शिक्षक हो या सरकारी कर्मचारी स्वयं के बालक बालिकाओं का प्रवेश सरकारी विद्यालय में अनिवार्यतः करवाया जाए। ताकि अनुकरण ही प्रेरणा बन सके। अन्यथा “गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज” वाली कहावत लागू होती हैं। और अभिभावकों के दृष्टिकोण को बदलना मुश्किल काम है तथा जब सर्वोच्च पदाधिकारी द्वारा धरातल विद्यालय स्तर (विद्यार्थी स्तर) से प्रतिपुष्टि ना हो तब तक वास्तविकता हीन शिक्षा कही जा सकती है। शिक्षा के हर पहलू को राजनीति के तथ्य से मुक्त होना चाहिए अन्यथा बदलाव की कतई गुंजाइश नहीं है।
लेखक का परिचय
नाम-गीता राम मीना
प्राध्यापक ( हिन्दी) स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल लाखेरी के.पाटन जिला बूंदी, राजस्थान।
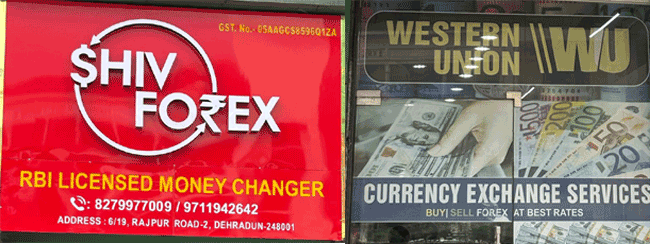










,?