टेलीफोन से पेजर और मोबाइल तक, लगाना नहीं था आसान और कटवाना भी मुश्किल
अक्सर छुट्टी का दिन हो तो सभी की यही कामना रहती है कि टेलीफोन की घंटी न बजे। साथ ही मोबाइल भी शांत रहे। किसी बारे में सोचना और व्यवहारिकता में काफी फर्क है।
 अक्सर छुट्टी का दिन हो तो सभी की यही कामना रहती है कि टेलीफोन की घंटी न बजे। साथ ही मोबाइल भी शांत रहे। किसी बारे में सोचना और व्यवहारिकता में काफी फर्क है। कई बार तो छुट्टी के दिन सुबह-सुबह ही फोन व मोबाइल घनघनाने लगते हैं। ऐसे में कई बार पूरा दिन भागदौड़ में ही बीत जाता है। सुबह तड़के आने वाले फोन ज्यादातर अप्रिय समाचार वाले ही होते हैं। ऐसे में सुबह के समय फोन की घंटी न बजे। यही मैं अक्सर सोचता रहता हूं, लेकिन होनी पर किसका जोर है। जो होना हो तो होकर ही रहता है।
अक्सर छुट्टी का दिन हो तो सभी की यही कामना रहती है कि टेलीफोन की घंटी न बजे। साथ ही मोबाइल भी शांत रहे। किसी बारे में सोचना और व्यवहारिकता में काफी फर्क है। कई बार तो छुट्टी के दिन सुबह-सुबह ही फोन व मोबाइल घनघनाने लगते हैं। ऐसे में कई बार पूरा दिन भागदौड़ में ही बीत जाता है। सुबह तड़के आने वाले फोन ज्यादातर अप्रिय समाचार वाले ही होते हैं। ऐसे में सुबह के समय फोन की घंटी न बजे। यही मैं अक्सर सोचता रहता हूं, लेकिन होनी पर किसका जोर है। जो होना हो तो होकर ही रहता है।सच पूछो तो संचार के साधन जितने बढ़े उतना ज्यादा ही लोगों के पास वक्त कम हो गया। पहले न तो टेलीफोन थे, न ही टेलीविजन। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समाचार रेडियो व समाचार पत्रों से ही मिल जाते थे। परिचितों व नातेदारों की सूचना चिट्ठी से मिलती थी। छोटे में मुझे टेलीफोन देखने का सौभाग्य पिताजी के आफिस में ही मिला। आफिस हमारे घर से करीब पांच सौ मीटर दूरी पर स्थित था। वहां कुछ अफसरों के कमरों में फोन थे।
मैं बचपन से ही आफिस परिसर में घूमता रहता। अधिकतर अधिकारी व कर्मचारी मुझे पसंद करते थे। किसी को मैं अंकल कहता और किसी को भाई साहब। मेरी इच्छा होती कि टेलीफोन से किसी से बात करूं, लेकिन किससे करूं यह मैं नहीं जानता था। जब कोई फोन से बात करता तो मैं उसके बगल में खड़ा होकर यह जानने की कोशिश करता कि दूसरी तरफ से कैसी आवाज आ रही है।
हां तब हम बच्चे टेलीफोन का खेल भी खेला करते थे। माचिस की डिब्बी से दो टेलीफोन बनाते। दोनों का संपर्क लंबे धागे से जोड़ते। फिर काफी दूरी पर एक बच्चा उसमें बोलता और दूसरा बच्चा कान पर लगाता। धागे से आवाज की तंरगे फोन रूपी एक डिब्बी से दूसरी डिब्बी तक पहुंचती। अस्पष्ट सा कुछ-कुछ सुनाई देता और हम खुश होते कि बच्चों के पास भी टेलीफोन है।
उन दिनों दुख की घटना का समाचार तार से भेजा जाता था। किसी के घर तार पहुंचा तो समझो उस परिवार पर कोई विपदा आ गई हो। वहीं, टेलीफोन से भी समाचार दिए जाते, लेकिन इसके लिए फोन करने वाले व सुनने वाले को भी उसकी कृपा दृष्टि चाहिए होती, जिसके पास फोन है। मसलन पिताजी के आफिस में कई बार दिल्ली से बहन व जीजा का फोन आता। रिसिव करने वाला वाबू उठाता और फिर बात होती कि उन्हें बुला रहे हैं, कुछ देर बाद फोन करना। पिताजी को फोन की सूचना मिलती, तो उनके साथ मैं भी चला जाता। मेरी इच्छा होती कि मैं भी फोन से बात करूं। एकआध बार उन्होंने मुझे भी फोन थमाया, लेकिन क्या बोलूं, यह मुझे सूझता तक नहीं था।
नब्बे के दशक में संचार क्रांति ने तेजी से विकास किया। वर्ष 82 के दौरान रंगीन टेलीविजन घर-घर नजर आने लगे। 1990 के बाद से तो टेलीफोन भी घर-घर में दिखाई देने लगे। फिर भी टेलीफोन लगाना आसान नहीं था। इसके लिए बाकायदा बुकिंग होती थी। जब कागजी औपचारिकता पूरी हो जाती, तो दो से तीन साल फोन कनेक्शन जोड़ने में लगते थे।
कुछ शहरों में तबादलों को झेलकर वर्ष 99 में मैं वापस देहरादून आया। मैने भी फोन के लिए अप्लाई किया। तब भी घर में फोन लगाने में दो से तीन माह लग रहे थे। मैने कागजी औपचारिकताएं एक दिन में ही पूरी कर ली। बुकिंग कराई और सिकियोरिटी की राशि भी जमा करा दी। फोन सिफारिशी व कोटे का था। ऐसे में तब सिर्फ एक्सचेंज से ही एक लाइनमैन ने घर आकर कनेक्शन जोड़ना था। एक दिन में सारा काम पूरा होने के बाद मामला जूनियर इंजीनियर स्तर पर पहुंचा। वह काफी घाघ था। इंजीनियर मुझसे पैसे चाह रहा था, लेकिन मैं रिश्वत से खिलाफ था।
इंजीनियर ने जो काम एक दो दिन में करना था, उसे टालते हुए उसने तीन दिन लगा दिए। इस पर मैने उसे रिश्वत लेते गिरफ्तार करने की योजना बनाई। वह पांच सौ रुपये मांग रहा था। मैं उसे सीबीआई से पकड़वाना चाह रहा था। इसका जिक्र मैने अपने एक परिचित से भी कर दिया, जो टेलीफोन एक्सचेंज में ही कार्यरत था। एक रात मैं जब आफिस से घर पहुंचा दो देखा कि टेलीफोन लगा हुआ है। हालांकि उसमें करंट नहीं दौड़ रहा था। घर में मैने पूछा कि इंजीनियर ने पैसे तो नहीं मांगे। इस पर पिताजी ने ना मे जवाब दिया। शायद परिचित ने ही इंजीनियर को आगाह कर दिया था। खैर अगले दिन फोन में करंट भी दौड़ गया।
उन दिनों मोबाइल रखना कुछ ही लोगों के बूते की बात थी। ऐसे में घर का फोन ही सबकुछ था। तब पेजर का भी कुछ समय तक एक दौर चला। क्राइम देखने के दौरान मुझे ऑफिस से पेजर दिया गया। उसे बड़ी शान से मैं भी बेल्ट में फंसा कर रखता था। पेजर का एक नंबर होता था, जो सिर्फ शहर के भीतर ही काम करता था। मेरे पेजर का नंबर 302 था। मुझसे यदि किसी को संपर्क करना होता था तो वह लैंडलाइन से कंपनी को फोन करता था। वहां आपरेटर को बताया जाता कि 302 में ये मैसेज भेज दो। अक्सर पेजर में मैसेज भेजने वाले का नाम और लैंडलाइन का कांटेक्ट नंबर का मैसेज आता। मैसेज पढ़ने के बाद यदि जरूरत हो तो कहीं लैंडलाइन से उस नंबर पर बात कर ली जाती। पेजर की भी अपनी सीमाएं थी। एक बार मैं सहारनपुर स्थित ससुराल जा रहा था। शोक से पेजर भी साथ ले गया। मोहंड के जंगल से पहले ही पेजर बंद हो गया और एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं था।
तब कई स्थानों पर टेलीफोन के ऐसे बूथ थे, जिसमें एक रुपये का सिक्का डालकर बात हो जाती थी। जुगाड़ तंत्र यहां भी था। कई लोग घंटी बजने के बाद सिक्का डालने की बजाय रिसीवर के उस स्थान से बोलते थे, जो सुनने के लिए होता है। ऐसे में दूसरी तरफ आवाज साफ पहुंच जाती थी और सिक्का नहीं डाला जाता था। ऐसे ही कई लोग फ्री में काम चलाते थे। खैर मेरे से लिए पेजर में घर के मैसेज कुछ ऐसे आते थे-घर का बल्ब फ्यूज हो गया है। शाम को घर आते समय रास्ते से बल्ब खरीदकर ले आना।
हमारा ये लैंडलाइन फोन काफी साल तक आस-पड़ोस के लोगों के लिए भी संचार का सुविधाजनक सहारा बना रहा। पड़ोसियों ने मेरे नंबर इतने लोगों को बांटे थे, जितने शायद मैने भी नहीं बांटे। मेरे फोन कम और लोगों के ज्यादा ही आते थे। खैर रात के 12 बजे तक भी मैने लोगों की फोन में बात कराई। जब ज्यादा परेशान हो जाता तो मैं यही सोचता कि कब इन फोन से छुटकारा मिलेगा। फिर जब मोबाइल क्रांति का दौर शुरू हुआ तो धीरे-धीरे लैंड लाइन पर लोगों के फोन आने बंद हो गए। जब लैंडलाइन फोन कभी कभार ही बजने लगा तो मैने कनेक्शन कटवा दिया।
कनेक्शन काटना जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। वर्ष 2020 में मैने कनेक्शन काटने का फार्म भर दिया। टेलीफोन को विभाग में दे दिया। इसके बावजूद भी फोन कई दिन बाद ही काटा गया। वहीं, इसका बिल मुझे तब तक का आ गया, जब तक उससे करंट नहीं काटा गया। ऐसे कई उदाहरण थे, जब लोगों को फोन कटाने के बाद भी बिल भेजे जाते रहे। अब मुझे कनेक्शन लेने के दौरान जमा की गई सिक्योरिटी राशि की वापसी का इंतजार है, जो कहीं फाइलों में दो साल से धूल फांक रही है।
मोबाइल का कोई समय नहीं है। कभी परिचित की काल, तो कभी मिस काल। जब ये भी न हो तो तब किसी कंपनी का मैसेज कि मैं एक करोड़ डालर जीत गया हूं। फोन की जो घंटी बचपन में मुझे अच्छी लगती थी, अब उसे सुनकर कई बार गुस्सा आता है, लेकिन फोन है तो बजेगा ही। अच्छी खबर भी आएगी और बुरी भी।
भानु बंगवाल





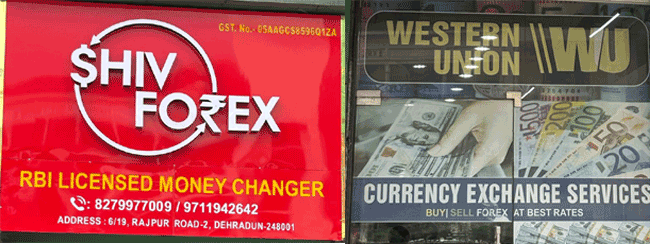

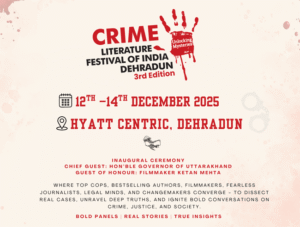





“टेलीफोन से पेजर और मोबाइल तक, लगाना नहीं था आसान और कटवाना भी मुश्किल”।
भानु बंगवाल जी आप द्वारा किया गया विश्लेषण बहुत ही सूंदर है, लेख पड़ कर ऐसा लग रहा है जैसे अपने बचपन की सच्चाई किसी के मुँह से सुन रहे है।