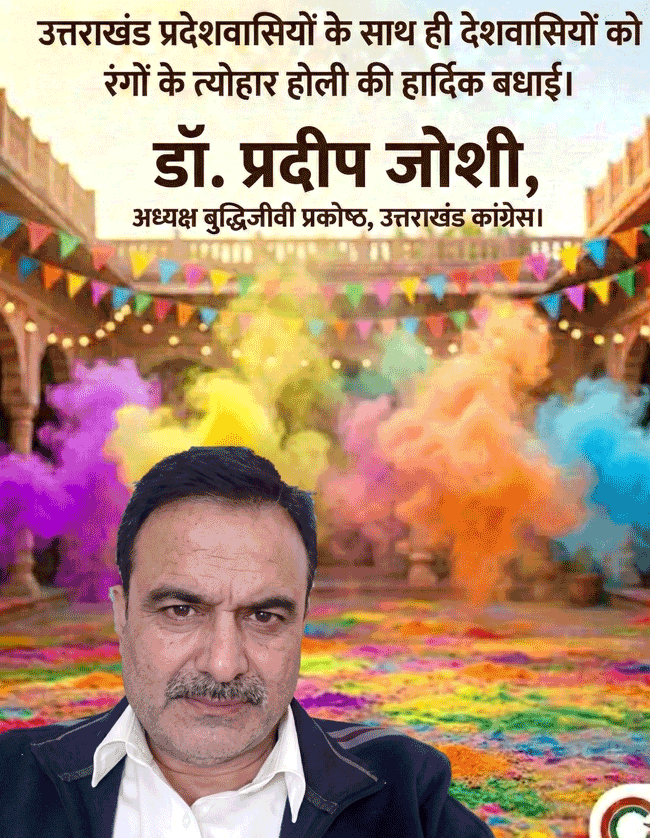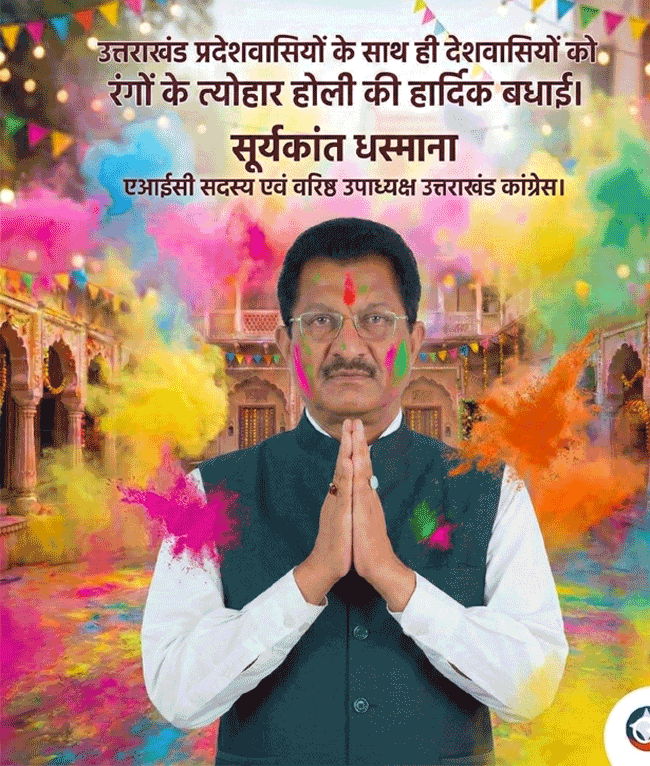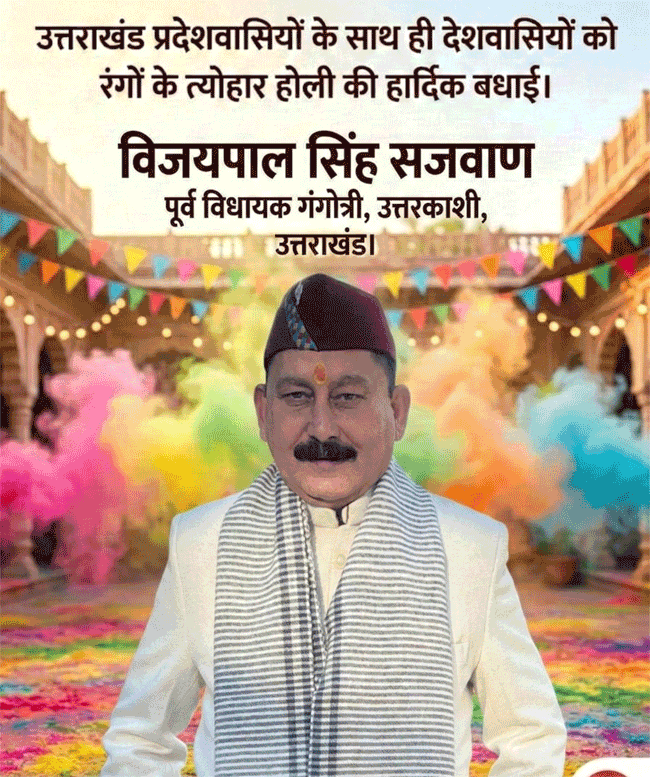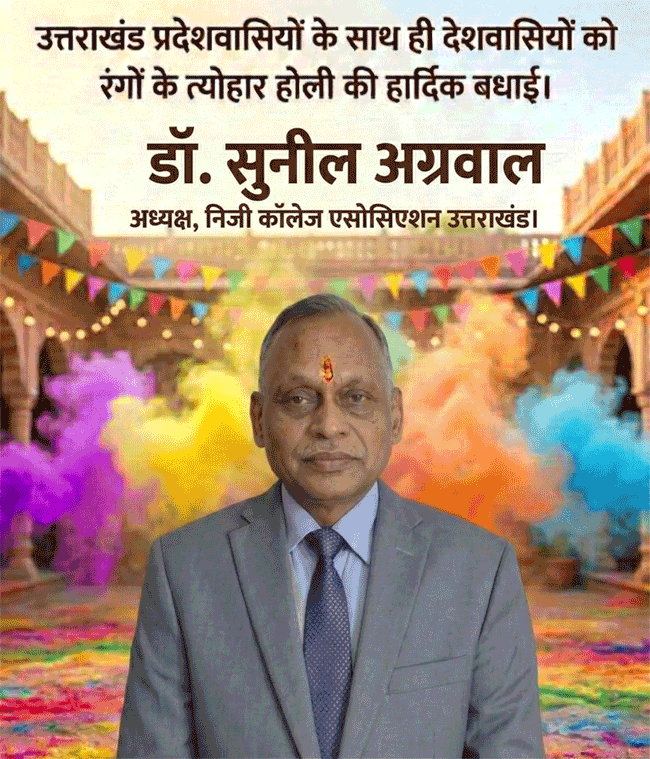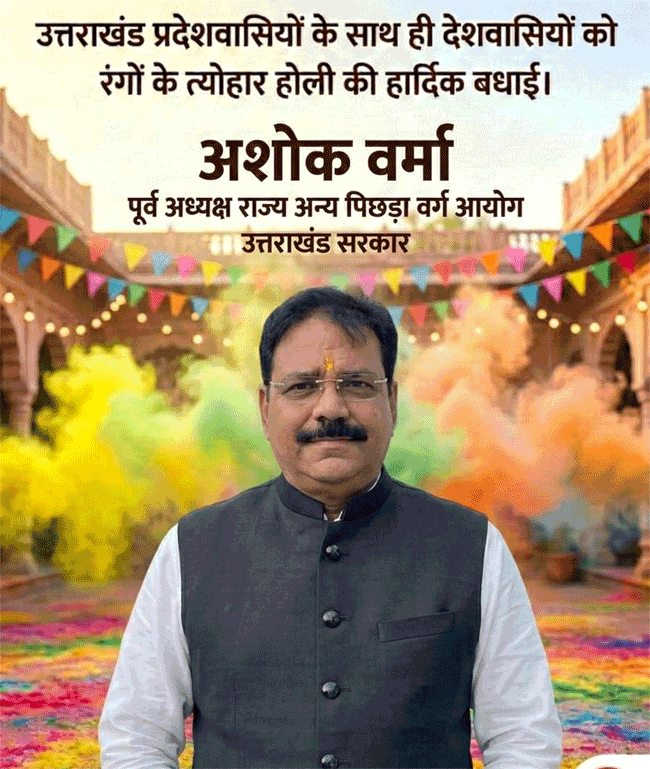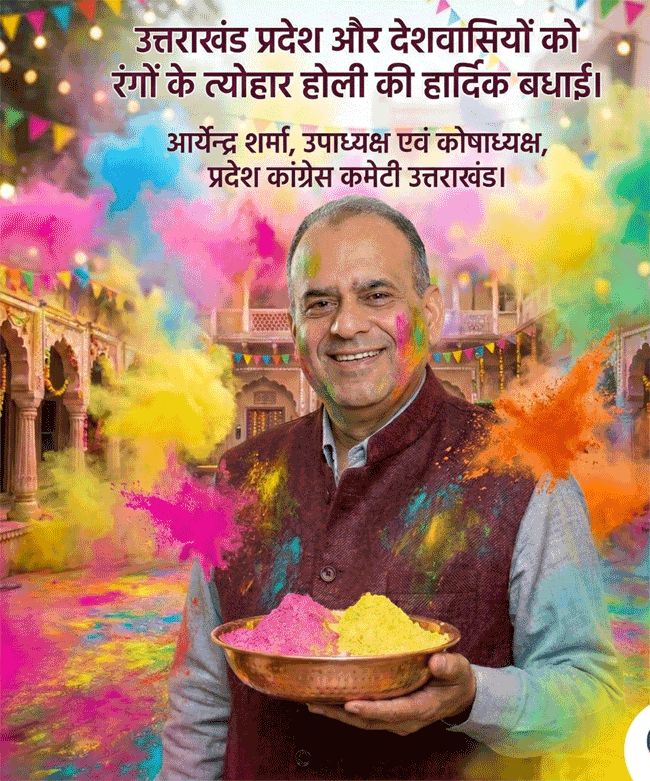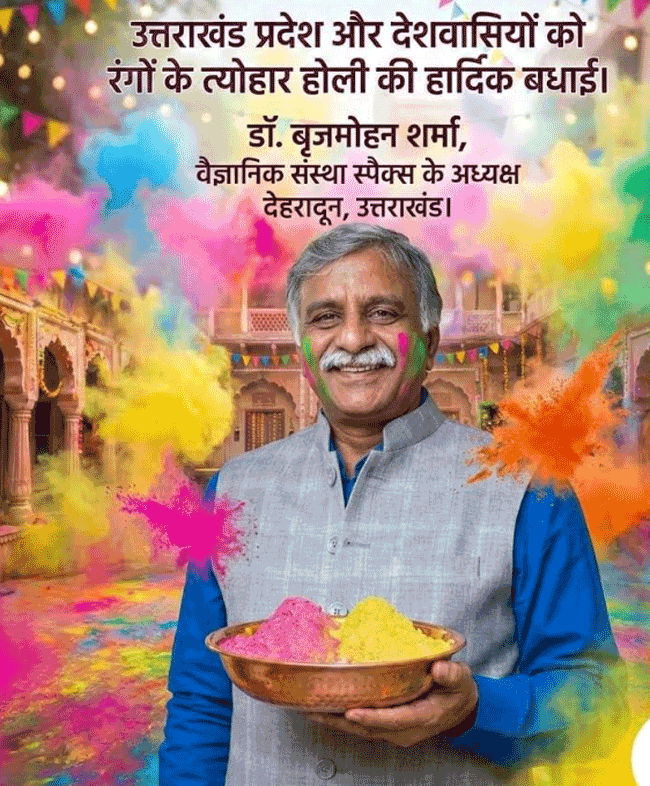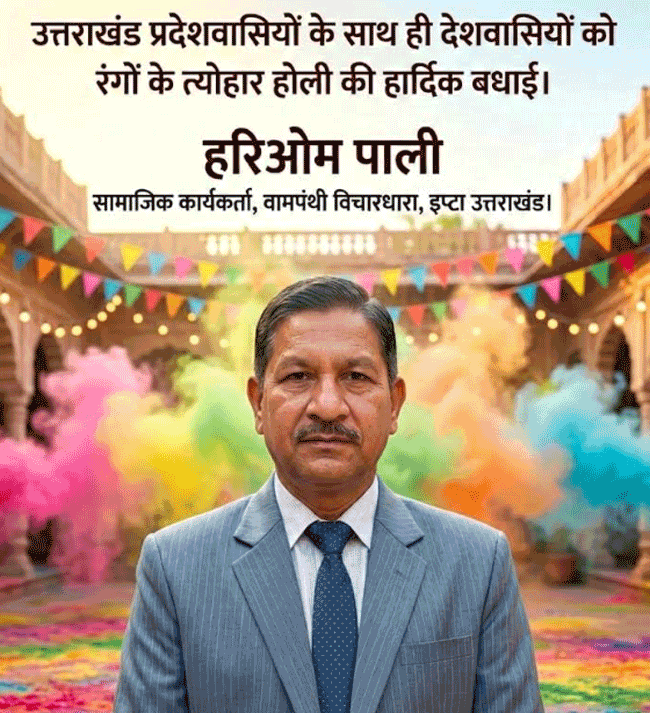दृष्टि दिव्यांग डॉ. दयाल सिंह पंवार का लेख- भारतवर्ष की परम्परा तथा आधुनिकता का समीकरण
भारतवर्ष एक अत्यन्त प्राचीन एवं पारम्परिक राष्ट्र है। साथ ही हमारा देश अत्यन्त तरुण और आधुनिक भी है। आलोचक हमारे इस कथन में विरोधाभास का अनुभव कर सकते हैं। कालक्रम की दृष्टि से अत्यधिक प्राचीन होने के कारण विभिन्न परम्पराओं और संस्कारों ने हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय जीवन को समृद्ध बनाया है। इतना ही नहीं हमारे राष्ट्रीय जीवन के सभी पक्ष परम्परा से अनुप्राणित हैं। आधुनिककाल में विशेष रूप से विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में होने वाली प्रगति के कारण कुछ क्षेत्रों में तो इस काल को आधुनिकोत्तर भी कहा जाने लगा है। इस भौतिक तथा वैज्ञानिक प्रगति के परिणामस्वरूप मानवीय मूल्योंए परम्पराओं, संस्कारों आदि के विषय में अनेक प्रश्न खड़े किए जाने लगे हैं। परम्परा और आधुनिकता में दिखाई देने वाला अन्तर्विरोध कितना वास्तविक है? क्या पाश्चात्यीकरण और आधुनिकीकरण की अवधारणा एक ही है या भिन्न? क्या आधुनिक दिखाई देने के लिए अपनी श्रेष्ठ परम्परा भी त्याज्य है? क्या प्राचीन होने के कारण ही कोई परम्परा उपादेय है? आज के सन्दर्भ में ये प्रश्न महत्त्व पूर्ण हैं अतः इनका हल खोजने का प्रयत्न अवश्य किया जाना चाहिए।
आधुनिक परिवेश के अनुकूल न होने के कारण हम अनेक परम्पराओं को तिलांजलि देते हैं और कभी उन में समयानुकूल परिवर्तन करते हैं। कभी कभी अपने को अधिक सभ्य, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, आधुनिक और विशिष्ट सिद्ध करने के लिए हम अपनी श्रेष्ठ परम्पराओं का अनादर भी करते हैं। यदि अविवेक के साथ परम्परा को ढोना अनुचित है तो दुराग्रह के साथ अपनी भव्य परम्परा का त्याग और अनादर भी अपराध है। आधुनिक नूतन परिवेश में परम्पराओं की परीक्षा के विभिन्न पक्ष वर्तमान सन्दर्भ में अत्यधिक प्रासंगिक हैं। हमारे समाज का यह वैशिष्ट्य है कि समय समय पर प्राचीनकाल से हम इन विषयों पर विचार करते रहे हैं। उदाहरण स्वरूप काव्य की उत्कृष्टता तथा अपकृष्टता के सन्दर्भ में कविकुलगुरु कालिदास के द्वारा सूत्र रूप में प्रकट किया गया यह उद्गार यहाँ पर भी चरितार्थ होता है। यथा—
पुराणमित्येव न साधु सर्वम्ए
न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्य
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्भजन्तेए
मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः।
अर्थात् कोई काव्य केवल पुरातन होने के कारण ही श्रेष्ठ नहीं होता और न ही नया होने के कारण वह निन्दनीय होता है। सज्जन परीक्षा के बाद ही यह तय कर पाते हैं। ऐसे विषयों में में मूढजन ही दूसरों के निर्णय के आधार पर निर्णय लेते हैं। परम्परा तथा आधुनिकता सम्बन्धी ये विभिन्न पक्ष तथा आज घटित होने वाली विभिन्न घटनाएं निश्चय ही विषय पर चर्चा के औचित्य को सिद्ध करती हैं।
परम्परा का स्वरूप या प्रकृति
केवल कुछ कालखंड तक निरन्तर एक ही रूप में दोहराई जाने वाली गतिविधि का नाम ही परम्परा नहीं होता। यह सही है कि कुछ काल तक चलते रहना परम्परा का स्वभाव होता है किन्तु यह भी उतना ही सच है कि युग-धर्म की आवश्यकता के अनुसार उस में परिवर्तन स्वाभाविक होता है और शायद उसकी यही विशेषता उसे रूढ़िवाद से भिन्न बनाता है। होलीए दीवालीए दशहरा जैसे पर्व जो एक दीर्घकाल से भारतीय परिवेश को आह्लादित करते आ रहे हैंए उन में भी समय-समय पर विभिन्न परिवर्तन आए हैं और स्थानीय परिवेश के अनुसार उनकी आयोजन-पद्धति में भी भिन्नता स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो परम्पराएं आधुनिक परिवेश के प्रतिकूल हो जाती हैंए वे या तो स्वतः नष्ट हो जाती हैं या फिर समाज उन्हे समाप्त कर देता है। परम्परा की स्वीकृतिए उसके विस्तार या नूतन सन्दर्भ में अमान्य घोषित करने का भारी दायित्व समाज के प्रबुद्ध एवं शिक्षित वर्ग पर होता है। उस वर्ग की मानसिकता की इस दृष्टि से बड़ी भूमिका होती है। इस वर्ग का दायित्व है कि एक ओर समाज के लिए अभिशाप बनने वाली रूढ़ियों का विरोध करे तो दूसरी ओर भारतवर्ष की पहचानए आन बान और शान बनने वाली विरासत की रक्षा करे। दोनों कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और विशिष्ट है। दुर्भाग्य से दूसरे दायित्व की पढ़े-लिखे विशिष्ट लोगों ने बहुत उपेक्षा की है।
आधुनिकता की अवधारणा
आधुनिकता एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है और प्रत्येक काल में आधुनिक होने का विचार समकालीन समाजों में रहा है। रोचक बात यह है कि प्रायः विजेता या प्रभावशाली जाति या राष्ट्र द्वारा जिन मूल्यों, मान्यताओं और परम्पराओं को अपनाया जाता है, शेष विश्व के लिए वे ही आधुनिकता के मानदण्ड मान लिए जाते हैं। मध्यकाल में जब हम मुगलों के द्वारा आक्रान्त हुएए तब हमारी शिक्षा और संस्कृति पर उसका विशेष प्रभाव रहा और उर्दूए फारसी पढ़ना आदि आधुनिकता के लक्षण बने। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा आक्रान्त होने पर अंग्रेजी पढ़ना और अंग्रेजों के अनुसार आचरण करना आधुनिकता के लक्षण बन गए। आज के परिवेश पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट अनुभव हो जाता है कि पाश्चात्यीकरण को ही आधुनिकीकरण समझा जाने लगा। यह सही है कि आज विज्ञान का युग है और तर्कपूर्ण वैज्ञानिक चिन्तन आधुनिक समाज का महत्त्वपूर्ण बिन्दु उभरकर आया है। यह भी सही है कि वर्तमान भौतिक विकास में पाश्चात्य.देशों की अग्रगण्य भूमिका रही है किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वे हर क्षेत्र में अनुकरणीय माने जाएं।
भारतवर्ष की अपनी पहचान
हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भारतवर्ष एक प्राचीन किन्तु फिर भी तरुण राष्ट्र है। जैसे सूरज, चन्दा और तारे बहुत प्राचीन हैं किन्तु हर समय नवीन भी हैं। विश्व के बहुत सारे राष्ट्र हमारी अपेक्षा इस अर्थ में आधुनिक और नवीन हैं क्योंकि उनका जन्म ही बहुत अर्वाचीनकाल में हुआ है। अत्यधिक प्राचीन होने के कारण अनेक विशिष्ट परम्पराओंए मान्यताओं और मूल्यों का एक भव्य स्वरूप भारतीय मानस ने आत्मसात् किया। फलस्वरूप एक बहुआयामी संस्कृति ने विराट् रूप धारण करके भारतवर्ष को पहचान दी।
त्याग, तप, करुणा संयम तथा सहनशीलता आदि मानवीय मूल्य हमारे स्वभाव में हैं। फिर भी हाल में ही कुछ दुर्घटनाओं के आधार पर देश पर असहिष्णु होने के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों का ध्येय कुछ भी हो किन्तु इतना तो सिद्ध हो ही जाता है कि मानवीय मूल्यों की थोड़ी.सी भी उपेक्षा हमको सह्य नहीं है। हमने काल के अनेकों थपेड़ों को सहा है। हमारी मान्यताओंए मूल्यों, परम्पराओं और संस्कृति की बहुत परीक्षा हुई है। एक हजार वर्षों से आक्रान्त होने के बावजूद भी हमारे वे संस्कार अक्षुण्ण बने हुए हैं। भारतवर्ष के विषय में पूर्व राष्ट्रपति तथा प्रख्यात मनीषि डॉण् एसण् राधाकृष्णन का यह मन्तव्य उल्लेखनीय हैए श्आधुनिक यूनान प्राचीन यूनान से भिन्न है, आधुनिक मिस्र प्राचीन मिस्र से भिन्न है किन्तु आधुनिक भारतए जहाँ तक दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, मूल रूप से प्राचीन भारत से भिन्न नहीं है। फाहियान, ह्वेन्सांगए कीथ, मैक्समूलर, सिलवाँ लेवी जैसे विभिन्न विदेशी मनीषियों ने इस संस्कृति के विभिन्न पक्षों के वैशिष्ट्य की न केवल घोषणा की बल्कि उसके विविध पक्षों के अध्ययन में अपना जीवन समर्पित कर दिया।
परम्पराओं की प्रतीकात्मकता
परम्पराएं प्रतीकात्मक होती हैं तथा वे संदेश की वाहिकाएं भी होती हैं। अध्ययन-अध्यापन में रत हम सबका यह दायित्व है कि पहले स्वयं अपनी परम्परा के प्रतीकों और सन्देशों को समझें और फिर उनका प्रसार भी करें। यह आश्चर्य की अपेक्षा वेदना का विषय तो तब बनता हैए जब विश्वविद्यालय के कुछ पढ़े-लिखे नवयुवक उत्सव के रूप में इस राष्ट्र के टुकड़े-टुकड़े करने की कसमें खाते हैं और इस प्रकार के कृत्यों से अपने को अधिक बौद्धिक और विशिष्ट सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अपनी तार्किक प्रतिभा के बल पर प्रचलित परम्पराओं को अधिक नूतन और सार्थक रूप देने के स्थान पर अपनी कुण्ठित मानसिकता के बल पर उन्हें उलटने का प्रयास करते हैं। यदि रक्तबीज, महिषासुर, कंसए रावण के आतंक को आप सच नहीं मान सकते तो प्रतीकों के संकेतों को तो समझ ही सकते हैं, किन्तु प्रतीकों को उलटना कहाँ की बुद्धिमानी है? रावण-दहन के बाद दशहरे की एक सन्देश देने वाली परम्परा उत्सव के रूप में तैयार होती है और महिषासुर-वध के बाद भी वैसा ही पारम्परिक संकेतात्मक उत्सव मनाया जाना प्रारम्भ होता है। समाज के इन खल-नायकों के प्रति सहानुभूति उनके वध के बाद उनके परिवारजनों के तुष्टीकरण के लिए कदाचित् स्वाभाविक हो सकती है, किन्तु आज उनके परिवार के कौन लोग शेष हैं, जिनका हम तुष्टीकरण करना चाहते हैं? डैविड फ्राले का यह कथन हमारे लिए ध्यान देने योग्य है कि भारत एक ऐसा विचित्र देश हैए जहाँ के लोग अपनी श्रेष्ठ परम्पराओं का परिहास करने में गौरव का अनुभव करते हैं।
अब समय आ गया है कि हम घर के ही चिराग़ से घर को आग लगाने की मानसिकता को छोड़ दें। पेड़ की जिस डाल पर बैठे हैं, उसी डाल पर कुल्हाड़ी चलाने से कालिदास बन जाने का ढोंग छोड़ दीजिए। शिक्षित एवं जागृत युवकों से यह अपेक्षा है कि वे अपने दायित्व को समझें तथा समाज को स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाएं। इसके लिए जड़ तथा अनुपादेय परम्पराओं के भार से समाज को मुक्त करना भी एक आवश्यक दायित्व है। हम जानते हैं कि पहले अँधेरे में चलते हुए लोग जलती हुई लकड़ियाँ हाथ में लेकर चलते थे। अब यदि वह बुझ गई है तो अन्य कोई प्रयोजन न होने के कारण त्याज्य है। एक महिला पूजा करते समय पालतू बिल्ली को इस लिए बन्द कर देती थी क्योंकि वह पूजा में बाधा उत्पन्न करती थी। उसकी बहू उसको ऐसा करते हुए देखती थी। जब उसकी सास न रही और उसने पूजा का क्रम बनाया तो वह किसी अन्य स्थान से बिल्ली लाती और पूजा के समय उसको बन्द कर देती। यानि उसने अपनी सास के आशय को न समझते हुए बिल्ली को बन्द करने को अपनी पूजा का एक अंग बना लिया। नूतन परिवेश में परम्परा के सन्देश और संकेत को समझने की आवश्यकता है।
कुरीतियों को उचित सिद्ध करने का प्रयास सर्वथा निन्दनीय है। हांए किसी सामान्य गतिविधि का कुरीति के रूप में परिवर्तन का अध्ययन और चिन्तन तो अवश्य होना चाहिए। जैसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करने वाले भारतीय परिवेश में कैसे बाल-विवाह की कुरीति आ गई? मध्यकाल में युद्धों की अधिकता के कारण यह उक्ति प्रसिद्ध हुई-
बारह बरस लौं सूकर जीवै तेरह बरस लौं जिये सियारए
बरस अठारह छत्री जीवै आगे जीवन को धिक्कार।
किशोरावस्था आते-आते तरुणों को युद्ध-भूमि में जाना पड़ता था अतः विवाह-संस्कार बाल्यावस्था में ही होने लगे। मध्यकाल में ही आक्रान्ताओं के द्वारा पराजित राज्य की महिलाएं अपनी इज्जत को बचाने के लिए अग्नि का आलिंगन कर लेती थी। परिणामस्वरूप सती-प्रथा जैसी कुरीतियों को धार्मिक ताने-बाने में बाँधने के प्रयास हुए। यदि यह हमारी नियत परम्परा होती तो महाराजा दशरथ की मृत्यु के बाद तीनों रानियाँ जीवित न रह पाती। इसी प्रकार कैसे एक सामान्य लोकाचार दहेज के रूप में परिवर्तित हो गयाए इसे भी समझा जा सकता है।
हमारे राष्ट्र को परम्परा का अवदान
कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हमारा आधुनिकीकरण ब्रिटेन के साम्राज्यवादी शासन का परिणाम है। हमारा मानना है कि हमारी परम्पराओं ने हमें शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और यहां तक कि आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में भव्य व्यवस्थाएं दी थीं। हमारे आधुनिकीकरण की एक स्वाभाविक चाल थी। यदि हमारे इस ताने-बाने को नष्ट न किया गया होता तो हम अपनी स्वाभाविक चाल से इससे अधिक आगे भी होते और आधुनिक भी होते। यह सच है कि हम परस्पर एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते और प्राप्त करते हैं किन्तु यह भी उतना ही ठीक है कि सीखने-सिखाने और आदान-प्रदान की यह प्रवृत्ति दुतरफा होती है इकतरफा नहीं। परम्परा से प्राप्त जिन योगए आयुर्वेद आध्यात्मिकता आदि विद्याओं का प्रसार हम आज गर्व और स्वाभिमान से कर पा रहे है, अगर हम आक्रान्त न होते तो अपने उत्कर्ष की हम कल्पना कर सकते हैं। केवल कल्पनाओं में जीने का हमारा आशय नहीं है। हमारा कहना तो यही है कि अपनी समृद्ध परम्पराओं का केवल संरक्षण ही नहीं अपितु आधुनिक परिवेश के साथ उनकी संगति बिठाकर उनका इस तरह संवर्धन हो, जिससे सम्पूर्ण मानव-जाति का कल्याण हो। डॉ. एस राधाकृष्णन ने भारत की आध्यात्मिक विरासत और सत्य-तत्त्व की चर्चा करते हुए कहा है कि यह केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु वैज्ञानिक और नैतिक होने के कारण सम्पूर्ण विश्व के लिए ग्राह्य है। वास्तव में परम्परा का आधुनिकता के साथ समीकरण बिठाना भारतीय मानस का स्वभाव है।
अनेक ऐसे साक्ष्य और प्रमाण हैं, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि अपनी परम्परागत पद्धतियों के आधार पर यह राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाए हुए था। समस्त विद्याओंए कलाओं और शिल्पों की एक समृद्ध परम्परा इस देश में रही है। विभिन्न ग्रन्थों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ऋषियों द्वारा विभिन्न विद्याओं और कलाओं का सृजन तथा गुरु-परम्परा से प्रसार हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में परम्परा ने क्या योगदान दियाए इस विषय पर चर्चा करना अधिक काल तथा स्थान की अपेक्षा रखता है।
आधुनिक-काल की कुछ घटनाओं के आलोक में भी अपनी समृद्ध ज्ञान.परम्परा पर दृष्टिपात किया जा सकता है। 1780 में हैदर अली से पराजित होने के बाद कर्नल कूट की नाक काट दिए जाने पर बेलगाम (कर्नाटक) के एक वैद्य द्वारा उसकी सफल शल्य चिकित्सा इत्यादि के प्रसंग 18वीं शताब्दी तक हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कर्ष को द्योतित करते हैं। शिवकर बापूजी तलपदे ने संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन करके विमान-शास्त्र का प्रयोग तथा परीक्षण के साथ अत्यधिक परिश्रम करके विमान तैयार किया और 1895 में महादेव गोविन्द रानाडे, गुजरात के राजा गायक्वाड़ जैसे सम्भ्रान्तजनों तथा हज़ारों नागरिकों की उपस्थिति में मुम्बई में चौपाटी के समुद्रतट पर उस विमान को 1500 फिट की ऊँचाई तक उड़ाया और सफलतापूर्वक पुनः उसे वापस ले आए। बाद में रैली ब्रदर्स नामक एक चतुर कंपनी ने उस निर्धन तथा सरल व्यक्ति से समझौता किया और बाद में धोखा दे दिया।
17 वर्षों तक भारत में प्रवास करने के बाद लॉर्ड मेकॉले ने 2 फरवरी 1835 में ब्रिटिश संसद में जो वक्तव्य दिया थाए उस में भारत के वैभव की भी पर्याप्त चर्चा उसने की थी। क्या भारत पर शासन करने की मानसिकता रखने वाले ब्रिटिश शासन के इस प्रकार के राजभक्त से यह अपेक्षा की जा सकती है कि भारतीय शिक्षा-पद्धति का उन्मूलन करके अंग्रेजी शिक्षा का बीजारोपण भारत के मंगल की भावना से किया गया होगा? विलियम डिगवी ने 17वीं शताब्दी में भारतीय परम्परागत उद्योग, कृषि और व्यापार की अत्यधिक प्रशंसा की थी। इसी प्रकार स्कॉटलैंड के मार्टिन इत्यादि अनेक लोगों ने भारत के पारम्परिक वस्त्र.निर्माण के कौशल तथा अन्य पारम्परिक शिल्पों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।
उपसंहार
कहा जा सकता है कि श्रेष्ठ परम्पराओं की स्वीकृति तथा आधुनिकता के परिवेश में अनुपादेय परम्परा का परित्याग भारतीय चिन्तन एवं संस्कृति का स्वभाव है। परम्परा और आधुनिकता का ऐसा समीकरण बना रहे, इसके लिए विद्या के क्षेत्र में लगे हुए जागृत जनों की विशिष्ट भूमिका है। आवश्यकता है कि इस भूमिका का अधिक जिम्मेदारी और तत्परता के साथ निर्वहण किया जाए। स्वातन्त्र्योत्तर भारत में अपनी श्रेष्ठ परम्पराओं के संरक्षण एवं संवर्धन से ही भूमण्डलीकरण की इस हवा में हम अपनी पहचान को अधिक सावधानी के साथ सुरक्षित रख सकते हैं। श्वसुधैव कुटुम्बकम्श् या श्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्श् का जो आत्मीयता का अमृत विश्व को भारतवर्ष ने पिलाया थाए त्याग के साथ भोग का जो सार्वभौमिक पाठ हमारे ऋषियों ने विश्व को पढ़ाया था, उसका एक नया और भिन्न संस्करण भूमण्डलीकरण के रूप में आधुनिकता के नए चमकते हुए पात्र में हमें पिलाया जा रहा है। भूमण्डलीकरण की इस प्रवृत्ति का हमें सावधानी के साथ परीक्षण करने की आवश्यकता है। इस अवस्था में कुछ दबंग राष्ट्रों के हावी होने की पर्याप्त सम्भावना है। अतः पहचान खोने का संकट अनेक स्तरों पर अनेक राष्ट्रों पर रहता है। ऐसी परिस्थिति में हमारा पारम्परिक एवं सांस्कृतिक परिवेश ही हमारा रक्षा.कवच हैए जिसका सदा आधुनिकता के साथ समन्वय होता रहता है।
भूमण्डलीकरण के युग में यदि अपनी पहचान नहीं है,
स्वाभिमान औ देश.भक्ति का यदि जीवन में स्थान नहीं है,
यदि यान्त्रिक जीवन में अपनी परम्परा का मान नहीं है,
तब तो यह सचमुच इंडिया है भारत हिन्दुस्तान नहीं है।
लेखक का परिचय
नाम-डॉ. दयाल सिंह पंवार
लेखक व्याकरण विभाग, श्री लाल बहादुर संस्कृति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वह सक्ष्म संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एआइइपीवीटी देहरादून की एक्टिव काउंसिल के सदस्य हैं। हिंदी और संस्कृत में वह कविताएं लिखते हैं। साथ ही विभिन्न क्रियाकलापों में उन्हें सौ से अधिक बार सम्मानित किया जा चुका है। लेखक दृष्टि दिव्यांग हैं।