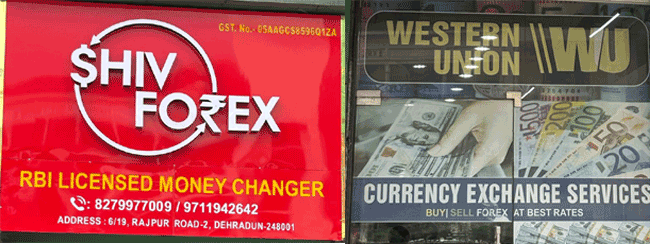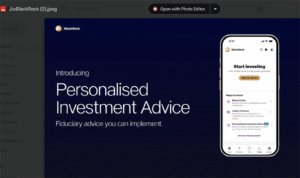विश्व ओजोन दिवस आज, जानिए इसे मनाने के कारण, सरल भाषा में पढ़ें इसकी सुरक्षा के उपायः डॉ. अशोक कुमार अग्रवाल
डा. अग्रवाल उत्तराखंड में देहरादून निवासी हैं। वह वर्तमान में उत्तरकाशी जिले के राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ में वनस्पति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।
 आज यानी 16 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का आयोजन करने की मुख्य वजह है कि ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान की और ध्यान केंद्रित करना है। यदि हम ओजोन परत को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो समूची धरती को खतरा पैदा हो जाएगा। इसकी सुरक्षा के बगैर धरती में जीव जंतु, पेड़-पौधों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए हम इसे सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि ओजोन परत धरती के लिए कैसे उपयोगी है।
आज यानी 16 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का आयोजन करने की मुख्य वजह है कि ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान की और ध्यान केंद्रित करना है। यदि हम ओजोन परत को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो समूची धरती को खतरा पैदा हो जाएगा। इसकी सुरक्षा के बगैर धरती में जीव जंतु, पेड़-पौधों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए हम इसे सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि ओजोन परत धरती के लिए कैसे उपयोगी है।ओजोन परत का कार्य
हमारे वायुमंडल में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ओजोन गैस से निर्मित एक घना आवरण है। इसे समताप मडंल (स्ट्रेटोस्फीयर) कहते हैं, जो ओजोन परत के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन परत सूर्य के प्रकाश में निहित पराबैंगनी किरणों को अपने में सोख लेती है। साथ ही पृथ्वी पर मानव सहित अन्य जीवधारियों की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से रक्षा करती है। इसी कारण ओजोन परत को ‘जीवन रक्षक छतरी’ या ‘पृथ्वी का सुरक्षा कवच’ भी कहते हैं।
ओजोन परत को पहुंच रहा है नुकसान
ओजोन परत में क्षय होने का सर्वप्रथम पता जोसेफ फोरमैन नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक को मई 1985 में उस समय लगा, जब वह ब्रिटिश अंटार्कटिका दल का नेतृत्व कर अंटार्कटिका क्षेत्र में अन्वेषण कर रहा थे। फोरमैन ने बताया कि अंटार्कटिका क्षेत्र के ऊपर ओजोन छतरी में एक बड़ा छेद है। नासा ओजोन ट्रेंड पैनल ने सन 1988 में अपनी एक रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि ओजोन का क्षय केवल अंटार्कटिका के ऊपर ही नहीं हो रहा, वरन ओजोन परत का अधिकांश भाग इस क्षय की चपेट में आ गया है। इससे ओजोन स्तर में सर्वव्यापी अल्पता आती जा रही है।
ओजोन परत के क्षय के कारण
ओजोन परत में प्राकृतिक रूप से जितना क्षय होता है, उतना ही उसका निर्माण भी हो जाता है। इससे समताप मंडल में स्थित ओजोन परत में संतुलन कायम रहता है। पिछले लगभग 70 वर्षों में वायुमंडल में ओजोन विनाशक गैसों की मात्रा इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ओजोन परत में विनाश की दर उसके निर्माण की दर से कहीं अधिक हो गई है। वर्तमान में सभी वैज्ञानिक इस तथ्य के संदर्भ में एकमत हैं कि ओजोन गैसों के क्षयीकरण के लिए मुख्य रूप से हेलोजनित गैसें उत्तरदाई हैं। इन गैसों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, हेलोजैन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख हैं। इनमें से ओजोन का प्रमुख शत्रु क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) है। इसका उपयोग हम बड़ी मात्रा में रेफ्रिजरेटरो, एयर कंडीशनर तथा एयरोसोल स्प्रे में करते हैं।
वनों का सफाया भी है कारण
ओजोन परत के क्षय का दूसरा प्रमुख कारण विस्तृत स्तर पर किया जा रहा वनोन्मूलन है। वनों का सफाया करने से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में निरंतर कमी हो रही है। इससे ओजोन निर्माण की दर में भी कमी आती जा रही है। वस्तुतः वनोन्मूलन ओजोन गैस का क्षय नहीं करता, वरन इससे ओजोन गैस का निर्माण नहीं हो पाता है। वर्तमान में अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं विभिन्न देशों के उपग्रह भी जब ओजोन परत से होकर गुजरते हैं, तो अभी ओजोन स्तर से ओजोन के अणुओं का विखंडन कर उसका क्षय करते हैं। सीएफसी के बाद मिथाइल ब्रोमाइड नामक रसायन ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है। मिथाइल ब्रोमाइड का उपयोग मुख्यतः निर्यातक वस्तुओं को लंबे समय तक सुगंधित रखने तथा कुछ कृषि फसलों की उत्पादकता को कायम रखने के लिए किया जाता है।
ओजोन परत के क्षय से उत्पन्न दुष्परिणाम
इसमें संदेह नहीं है कि ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं आने देती। वर्तमान में मानव ने अपने सुरक्षा कवच ओजोन परत को अपने अविवेकपूर्ण क्रियाकलापों से क्षत-विक्षत कर दिया है। यदि वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर को पूर्णता समाप्त कर दिया गया तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें बिना किसी रूकावट के पृथ्वी की सतह पर आ जाएंगी। इससे पादप जगत की प्रकाश संश्लेषण क्रिया अवरुद्ध होने से पेड़ पौधे समग्र रूप से नष्ट हो जाएंगे। पेड़ पौधों के समाप्त होने से वायुमंडल में ऑक्सीजन में विश्वव्यापी कमी होने लगेगी, जिसके प्रभाव से पृथ्वी का समस्त जैव जगत प्रभावित होगा। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से मानव के शरीर की त्वचा तथा आंखों की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगेगी। इससे मानव के शरीर में त्वचा का कैंसर तथा आंखों की बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यही नहीं पराबैंगनी किरणें मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कमजोर करती है, जिसे कारण मानव समुदाय मे ओजोन परत के क्षय से संक्रमण जनित बीमारियां व सांस संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ेगी।
ओजोन परत की सुरक्षा के उपाय, क्या हो रहे प्रयास
ओजोन परत के क्षय से उत्पन्न दुष्परिणामों की भयानकता से आतंकित मानव अब ओजोन परत की सुरक्षा के लिए प्रयासरत हैं। ओजोन परत की सुरक्षा का एकमात्र उपाय है, वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को सीमित करना। इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विश्व के विभिन्न देशों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कनाडा के मैट्रियल नगर में विश्व के 40 देशों में एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ, जिसमें सन 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन की दर को 50 फीसद कम करने का निर्णय लिया गया था। इस समझौते पर उस समय भारत चीन तथा ब्राजील को छोड़कर विश्व के 40 औद्योगिक रूप से विकसित देशों ने हस्ताक्षर किए थे। एक जनवरी 1989 को यह प्रभावी हो गया जिसकी पहली बैठक मई 1989 में हेलसिंकी में हुई थी। भारत के संदर्भ में दलील थी कि विश्व की कुल क्लोरोफ्लोरो कार्बन उत्सर्जन में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन आर्थिक संगठन के देश जापान तथा रूस का योगदान कदम: 30, 29,11 तथा 7 फीसद का रहता है। ओजोन परत को नुकसान से बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण भी एक महत्वपूर्ण उपाय है।
भारत से सबसे कम नुकसान
भारत विश्व के क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन का 1 फीसद से भी कम भाग वायु मंडल में छोड़ता है। अतः ओजोन स्तर की सुरक्षा का सर्वाधिक उत्तरदायित्व उन्हीं देशों का होना चाहिए, जो वायुमंडल में सर्वाधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ते हैं। इससे पूर्व मार्च 1979 में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में, मार्च 1990 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में, सन 1992 में ब्राजील की राजधानी रियोडीजेनेरो में तथा 1998 में कनाडा के मैट्रियल नगर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यावरण सम्मेलनों का आयोजन कर ओजोन स्तर की सुरक्षा के संबंध में अनेक प्रस्ताव पारित किए गए। ओजोन स्तर के बचाव के लिए केवल सम्मेलन आयोजित करना व प्रस्ताव पारित करना ही पर्याप्त नहीं है। वरन इन प्रस्तावों पर सभी देशों द्वारा कड़ाई से अमल करना अधिक महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ओजोन परत के अस्तित्व को बचाए रखने तथा इस परत के संरक्षण के लिए विश्वव्यापी जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है।
ओजोन संरक्षण पर भारतीय कानून
भारत ने सितंबर 1998 मैं मेंट्रियल समझौते का अनुपालन करते हुए वर्ष 2000 मैं ओजोन क्षति पदार्थ कानून लागू किया है। इस कानून के अनुसार 1 जनवरी 2013 के बाद चिकित्सा कार्यों को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में सीएफसी गैस का प्रयोग देश में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस कानून के अंतर्गत ओजोन क्षति पदार्थों का व्यापार करने वालो के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। मटेरियल समझौते के अनुसार ओजोन क्षति पदार्थों की प्रति व्यक्ति उपयोग की अधिकतम सीमा 300 ग्राम तक अनुमानित है, जबकि भारत में यह मात्रा अभी केवल 3 ग्राम प्रति व्यक्ति की है।

लेखक का परिचय
डा. अग्रवाल उत्तराखंड में देहरादून निवासी हैं। वह वर्तमान में उत्तरकाशी जिले के राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ में वनस्पति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।