यहां तीन गांवों में नहीं मनाते होली, जानिए उत्तराखंड में होली की विशेषता, पौराणिक और आज की होली में अंतर

जहां दशहरा शत्रु पर विजय का प्रतीक है। वहीं, होली स्वयं पर विजय का प्रतीक है। अपने राग, रंग, ईर्ष्या, विद्वेष जैसे अवगुणों (बुराइयों) को फाल्गुन की पूर्णिमा रात्रि में (ज्ञान के प्रतीक) में जलाकर, सुबह (उजाले में अपने अज्ञान का बोध) होने पर वैमनस्य को भूलकर, अपने मन से समाप्त कर, रंगों में (प्रेम व खुशी का प्रतीक) में भीगना ही होली है।
इतिहास के आइने में होली
ऋग्वेद (5/44/15) के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। यदि हम पृथ्वी की उत्पत्ति के महाविस्फोट सिद्धांत (Big Bang Theory)को ऋग्वेद की इस रिचा की व्याख्या के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण व तथ्यों को जोड़ते हुए देखें तो यह बात सत्य ही साबित होती है कि पृथ्वी सहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति अग्नि से ही हुई है। सनातन धर्म में इस घटना का दिन चैत्र प्रतिपदा माना जाता है। उससे पहले यज्ञ की अग्नि की तरह अपने अंदर के अवगुणों को (होली के दिन) जलाकर, शुद्ध होकर नये साल का स्वागत करने की तैयारी है।
महाद्वीप में किसी न किसी रूप में प्रचलित है होली
अगर आप विश्व भर का अवलोकन करें तो पायेंगे हर महाद्वीप के हर देश में होली का त्योहार किसी न किसी रूप में प्रचलित और मौजूद है। भले ही अपभ्रंश के चलते वह आज वर्तमान समय में किसी अन्य नाम व रूप में प्रचलित हो गया हो। कुछेक उदाहरणों से आप बात का मर्म समझ जायेंगे।
विश्व के उदाहरण
आपने योरोप (स्पेन) के टमाटर उत्सव (जिसमें एक स्थान पर एकत्र होकर एक – दूसरे को टमाटर फेंक कर मारे जाते हैं) जिसे La Tomatina कहते हैं। इसी प्रकार विश्व के अन्य देशों सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, तोबागो, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, फीजी में भी होली के ही आसपास होली से मिलते जुलते त्योहारों का आयोजन होता है।
पूरे भारत में मनाई जाती है होली
भारत की बात करें तो लगभग सम्पूर्ण भारत में थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ होली का त्योहार मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में इसे भगोरिया होली तो, बिहार में फगुआ, तमिलनाडु में वसन्तोत्सव व यौवन का त्योहार कमनपोडिगई के रूप में मनाया जाता है। ब्रज में यही त्योहार लठमार होली के नाम से विश्वविख्यात है। पंजाब में तो इस त्योहार की मस्ती देखते ही बनती है, यहां इस अवसर पर शक्ति प्रदर्शन की भी परम्परा है।
उत्तराखंड के कुमाऊं में होली
उत्तराखंड की बात करें तो कुमाऊँ की बैठकी होली, जो होली से लगभग एक माह पूर्व से शुरू हो जाती है। इसमें स्त्री व पुरुष मिलकर शास्त्रीय संगीत की धुनों पर झूमते हैं। विशेषता की बात यह है धीमे संगीत और स्थाई भाव के गीतों के साथ जब होली से एक सप्ताह पूर्व यही संगीत तेज धुन (चलती) में बदलकर माहौल में तेजी ले आता है तो इसे खड़ी होली कहा जाता है। खड़ी होली में स्त्री पुरूष खड़े होकर नाचने लगते हैं। होलिका दहन के दिन (चतुर्दशी तिथि) को कोरी होली तो (पूर्णिमासी की रात बीतने के बाद)दूसरी दिन की होली को गीली होली कहते हैं।
उत्तराखंड के गढ़वाल में होली
वहीं गढ़वाल बैठकी होली लगभग एक पक्ष पहले ( प्रतिपदा तिथि से ) शुरू होती है। इसमें बड़े बुजुर्ग एक स्थान पर बैठकर दादरा, ठुमरी जैसे गीतों का गायन करते हैं। अवयस्क (विशेषकर शैशवावस्था वाले बच्चे) एक झंडे के साथ टोली बनाकर ऐसे स्थानों पर जाते हैं, जहां वे राहगीरों को टीका लगाकर भेंट में कुछ धन (सिक्के या नोट) प्राप्त कर सकें।य ह क्रम होली के नजदीक आते नजदीकी गांवों में फेरी लगाने में बदल जाता है। होली के मुख्य दिन (गीली होली या बड़ी होली के दिन) अपने ही घर, गाँव के आसपास होली खेली जाती है।
पौराणिक और वर्तमान होली के बीच मुख्य अंतर
कुछ दशकों पहले जब मनोरंजन के लिए टीवी, मोबाइल जैसे गैजेट्स नहीं थे तो बच्चे बड़ी उत्सुकता से होली की तैयारी और इंतजार करते थे। परिवार के बड़े बुजुर्ग बच्चों के लिए बाँस की पिचकारी बनाते थे। परिवार की महिलाएं जंगलों से विभिन्न प्रकार के फूल बीन कर लाती थी, जिन्हें सिखाकर और ओखल में कूटकर रंग बनाये जाते थे। इन फूलों में सेमल के फूल से घोलने वाला रंग तैयार किया जाता था।
बाजारों में स्याही की टिकिया आ जाने के बाद बच्चों की ओर से इसका प्रयोग भिगोने वाले रंग के रूप में खूब किया जाने लगा। धीरे-धीरे बाजारों में विभिन्न कैमिकल युक्त रंग आ जाने पर प्राकृतिक रंग बनाना लगभग समाप्त सा ही हो गया है। बाँस से बनी पिचकारी तो मेड इन चाइना के यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स ने संग्रहालयों तक सीमित कर दी हैं। जो भी हो बहरहाल समय का प्रभाव हर चीज पर पड़ता ही है। वहीं प्रभाव हमारे आचार – विचार, रहन-सहन व तीज – त्योहारों पर भी पड़ना स्वाभाविक है।
कुछ ऐसे गांव भी हैं, जहां नहीं मनाई जाती है होली
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में तीन गांव ऐसे हैं जहां होली नहीं मनाई जाती। ऐसा नहीं कि उन गांवों के लोग होली के बारे में नहीं जानते, बल्कि वे होली मनाना नहीं चाहते हैं। आज से करीब पौने चार सौ साल पहले जम्बू कश्मीर से कुछ पुरोहित परिवार अपने यजमानों और कास्तकारों व मवेशियों के साथ रुद्रप्रयाग जनपद के क्वीली – कुरझण गांव में आकर बस गये थे।
ये लोग अपने घर – गृहस्थी के सामान के साथ अपनी ईष्ट देवी त्रिपुरा सुन्दरी की मूर्ति भी लाये थे। जिसे गांव में मन्दिर में मण्डुली बनाकर स्थापित कर दिया गया। त्रिपुरा सुन्दरी को होली का हुड़दंग पसंद नहीं है, यह मान्यता है। यही मान्यता चली आ रही थी कि लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व कुछ ग्रामीणों ने आसपास के लोगों को होली खेलने का मन बनाया और होली खेली। तब अचानक इसी क्षेत्र में हैजा फैल गया। इससे जान – माल की काफी हानी हुई। फिर यह मान्यता ऐसी प्रबल हुई कि अभी तक चली आ रही है। आज भी इस गांव के लोग अपने गांव में होली नहीं खेलते।

लेखक का परिचय
नाम- हेमंत चौकियाल
निवासी-ग्राम धारकोट, पोस्ट चोपड़ा, ब्लॉक अगस्त्यमुनि जिला रूद्रप्रयाग उत्तराखंड।
शिक्षक-राजकरीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय डाँगी गुनाऊँ, अगस्त्यमुनि जिला रूद्रप्रयाग उत्तराखंड।
mail-hemant.chaukiyal@gmail.com
Bhanu Bangwal
लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
वाट्सएप नंबर-9412055165
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।




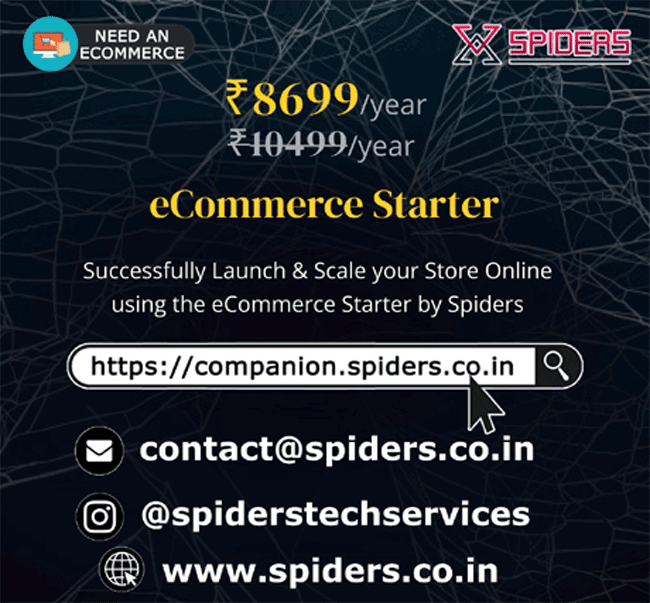
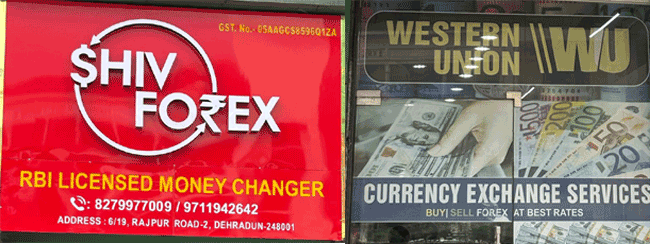


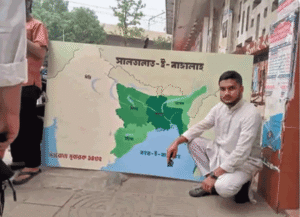




सुंदर जानकारी