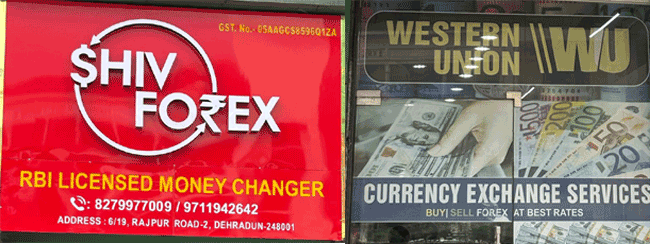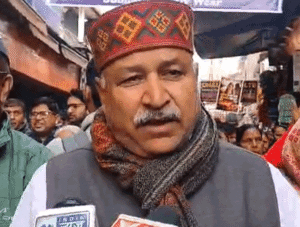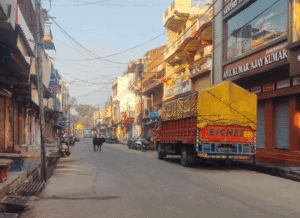उत्तराखंड के 13 जिलों में सबसे पुराना नगर है अल्मोड़ा, घास के कारण पड़ा अल्मोड़ा नाम, जानिए खासियत

उत्तराखंड के तेरह जिलों में अल्मोड़ा अधिक पुराना नगर है। नैनीताल और मसूरी की भाँति इसकी उत्पत्ति अंग्रेजों के आगमन पर नहीं हुई है। अल्मोड़ा नगर बसने से पूर्व यहाँ पर कत्यूरी राजा बैचल देव का अधिकार था। उन्होंने बहुत सी भूमि संकल्प करके गुजराती ब्राह्मण श्रीचंद तेवाड़ी को दे दी थी। कुछ समय पश्चात इस मंडल में चंद वंशीय राज्य स्थापित होने पर चंद राजाओं ने श्रीचंद की भूमि को अलग करके अपने महल निर्मित किये।
मानसखंड में अल्मोड़ा नगरी, जिस पर्वत पर बसी है, उसका वर्णन इस प्रकार है–
कौशिकी शाल्मली मध्ये पुण्यः कापाय पर्वतः ।
तस्य पश्चिम भागे वै क्षेत्र विष्णो प्रतिष्ठितम् ||
चंद शासनकाल में इसका नाम था राजापुर, फिर पड़ा ऐसे नाम
चंद शासनकाल में इसको राजापुर कहते थे। प्राप्त हुए ताम्रपत्रों में राजापुर लिखने का उल्लेख मिलता है। अल्मोड़ा के नामकरण के पीछे एक अम्लीय घास अल्मोड़ा का बहुतायत पाया जाना है। यह घास प्राचीनकाल में मंदिर के बरतनों को साफ करने के प्रयोग में लायी जाती थी। खसियाखोला के पुराने निवासी जिनको अल्मोड़िया कहते थे, प्रत्येक दिन अल्मोड़ा घास को कटारमल सूर्य मंदिर पहुँचाते थे।
हिेंदू राजाओं की राजधानी
अंग्रेजों के आगमन से पूर्व यह नगर कूर्मांचल के हिन्दू राजाओं की राजधानी था। सन् 1814-15 के नेपाल युद्ध के समय यहाँ गोरखों का राज्य था। इससे पूर्व यहाँ कूर्मांचल के चन्द्रवंशी राजा ही शासनारूढ़ थे। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि भूषण और मतिराम की कूमांचल दरबार में बड़ी प्रतिष्ठा थी। अंग्रेजों के आगमन पर भी अनेक वर्षों तक अल्मोड़ा ही कूर्मांचल की राजधानी रहा। एक समय यहाँ एक अंग्रेज कमिश्नर प्रतिष्ठित थे, उनका नाम था हेनरी रैमजे। इन्हें स्थानीय निवासी ‘रामजी’ के नाम से जानते थे। रामजी साहब इतने लोकप्रिय थे कि इन्हें राजा भी कहा जाता था। इनके शासन का ढंग प्रान्त के अन्य कमिश्नरों से भिन्न था। यही कारण था कि ये इतने जनप्रिय हो गये कि इन पर नाना प्रकार की कथायें व गीत लिखे गये।
भौगोलिक स्थिति
अल्मोड़ा का भौगोलिक क्षेत्रफल 3139 वर्ग किलोमीटर है और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले की जनसंख्या 6,22,506 है। अल्मोड़ा पर्वत की पीठ पर बसा है। इसकी ऊँचाई 5200 फीट से लकर 5500 फीट तक है। काठगोदाम से इसकी दूरी 120 किलोमीटर है। अल्मोड़ा का मुख्य बाजार लगभग दो किलोमीटर लम्बा है। बाजार की सड़क तारकोल या सीमेन्ट से निर्मित न होकर पत्थरों की स्लेट से ढकी हुई है। पूर्व में वर्तमान छावनी के स्थान पर लाल मंडी थी। उस लाल मंडी में किला, राजमहल, तालाब तथा मंदिर आदि थे। किले को ही लालमंडी कहा जाता था। अब यह क्षेत्र फोर्ट मौयरा कहलाता है। लार्ड मौयरा के काल में ही नगर व किला अंग्रेजों के अधिपत्य में आया था।
चंद राजाओं का महल बाद में कचहरी में परिवर्तित
आज जहाँ कचहरी है, वहाँ कभी चंद राजाओं का मल्ला महल था और जहाँ पर अब चिकित्सालय व मिशन स्कूल हैं, वहाँ बन्दों का तल्ला महल था। अल्मोड़ा में शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने से पूर्व अंग्रेज अधिकारी व सेना सन 1839 तक हवालबाग में रहते थे। यह स्थान मात्र 3920 फीट ऊँचा होने के कारण अंग्रेजों ने इसे अपने अनुकूल न पाया। अतः विवश होकर अंग्रेज अधिकारी अल्मोड़ा प्रवेश कर गये तथा सेना को लोहाघाट व पिथौरागढ़ स्थानान्तरित कर दिया।
गोरखा पल्टन
सन 1815 में गोरखा पल्टन हल्द्वानी में नियुक्त की गयी। यह निजामत बटालियन कहलाती थी। सुब्बा जयकृष्ण उप्रेती ने इस फौज में बहुत से कुमाऊँनी भी भर्ती किये। यह फौज कमिश्नर कुमाऊँ के अधीन कार्य करती थी। कालान्तर में यही कुमाऊँ बटालियन भी कही जाने लगी। सन 1846 में इसे लोहाघाट व पिथौरागढ़ से हटाकर
लालमंडी (फोर्ट मौयरा) में स्थापित किया गया। सन 1850 तक नागरिक सुरक्षा का कार्य फौज के सुपुर्द ही था। बाद में यह कार्य फौज से वापिस ले लिया गया। कुछ समय बाद कुमाऊँनी सैनिक, गोरखा फौज से अलग कर लिये गये। अब यह विशुद्ध रूप से गोरखा पल्टन कहलायी। अल्मोड़ा इसका घर बनाया गया।

पहले बहुतायात में थे नौले (चश्मे)
सन 1874 से पूर्व यहाँ तीन सौ साठ नौले (चश्मे) थे। धीरे धीरे वनों का क्षेत्रफल घटने से अधिकतर सूख गये। रानीधारा, राजनौली, चम्फानौला, कपीने का नौला आदि आज भी प्रसिद्ध हैं । अल्मोड़ा के पास बल्ढौटी जंगल के नीचे एक पत्थरों को खान है। यहाँ से छत व आँगन के लिए तराशे हुए पत्थर निकलते हैं।
यहां अंग्रेजों और गोरखा सैनिकों में हुई था युद्ध
सिडौली के सुरक्षित जंगल में गोरखा राजाओं की गढ़ी देखने को मिलती है। गोरखा सैनिकों ने 1814 में अंग्रेजों के साथ यहाँ युद्ध किया था। युद्ध में गोरखा सैनिकों के साथ-साथ दो अंग्रेज अधिकारी भी मारे गये थे, जिनकी कब्र आज भी देखने को मिलती है।
स्यूनरी राजा का था राज्य
इस जिले में स्थित स्यूनरा नामक पट्टी में पूर्व में स्यूनरी जाति के राजा का राज्य था। उसका स्यूनरा कोट नामक किला अभी तक ध्वंसावशेष के में एक टीले पर है। उसके भीतर से पत्थर काटकर एक सुरंग नदी तक बनी है। सुरंग द्वारा पानी नदी से किले तक पहुँचाया जाता था। इस पट्टी में हीराडुंगरी नाम की एक चोटी है। कहावत है कि जौहरी, चंद राजा के दरबार में आया। उसने इस पहाड़ को खोदकर हीरे निकालने के उद्देश्य से एक आवेदन पत्र दरबार में दिया, पर कतिपय कारणों से यह आवेदन स्वीकृत न हुआ।
यज्ञ में चमत्कार की कहानी
अल्मोड़ा की उत्तरी दिशा में स्थित कलमटिया पर्वत में चंद राजाओं का शस्त्रागार था। उस काल में वहाँ कन्नौज से श्रीबल्लभ पाँडे राजा के निमन्त्रण पर पधारे थे। ये विद्वान होने के साथ-साथ तंत्र विद्या में भी महारत हासिल किये हुए थे। बल्लभ पाँडे की विद्वता से नाराज हुए राजकर्मचारियों ने राजा को यज्ञ कराने की सलाह दी और बल्लभ पाँडे को यज्ञ पूर्ण कराने का दायित्व सौंपा। एक षडयन्त्र के तहत कर्मचारियों ने लकड़ी के स्थान पर लोहे के डंडे यज्ञ के लिए भिजवाये, लेकिन पाँडे जी ने अपनी विद्या के प्रभाव से लोहे के डंडों से ही यज्ञ सम्पन्न कर डाला। यज्ञ सम्पन्न करते समय सम्पूर्ण पर्वत ही जलकर काला हो गया। तभी से उसका नाम कलमटिया पड़ा। यहाँ अब चोटी में काषायेश्वर महादेव तथा देवी के मंदिर बने हुए हैं।

बिनसर मंदिर की कहानी
बिनसर पर्वत की चोटी पर कलविष्ट का टूटा हुआ मंदिर है। इसी पर्वत में विनेश्वर महादेव का भी मंदिर है। इसे राजा कल्याण चंद ने बनवाया था। मंदिर के निकट पानी का स्त्रोत भी है, इसे गूल काटकर भकुंडा के भकुंडी अपने गाँव में ले जाना चाहते थे। रात को स्वप्न में महादेव जी ने कहा कि यहाँ का जल स्रोत कम है। अत: इसे न ले जायें। उनको पर्वत के मध्य से पानी प्राप्त होगा। तीसरे दिन ही पानी का स्रोत स्वयं फूट पड़ा। अतः इस पानी को वर का पानी अर्थात् देवता का आशीर्वाद कहते हैं।
गणनाथ पर्वत है रमणीक
बिनसर में सेठ जमनादास बजाज ने गाँधी सेवा संघ की ओर से शैलाश्रम खोला था, जिसे बाद में स्थानीय साहूकार ने खरीद लिया था। गणनाथ का पर्वत भी कम रमणीक नहीं है। यहाँ पर विनायक थल एक समतल भूमि है। इसके ऊपर गणनाथ एक गुफा में विराजमान हैं। यहाँ लोहा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है।
श्यामा देवी का प्रसिद्ध मंदिर
अल्मोड़ा के पूर्व में वानणी देवी तथा पश्चिम में श्यामा देवी का प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो अल्मोड़ा के रक्षक की तरह कार्य करती हैं। श्यामा देवी के समीप ही सीतलाखेत प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ पर बाबा हैडियाखान का बनाया हुआ सिद्धाश्रम भी है।

लोगों में रहती थी टहलने की प्रवृति
अल्मोड़ा 6500 फीट की ऊँचाई पर स्थित एक रमणीक नगर है। यहाँ के निवासियों में प्रात: व सांयकाल टहलने की प्रवृत्ति बड़ी प्रबल थी। पश्चिम की ओर लगभग दो किलोमीटर की दूरी में मुख्य सड़क इस प्रकार मोड़ लेती है कि एक कोण बन जाता है। यहीं तक अधिकतर टहलने वाले पहुँचते हैं, इस स्थान का नाम ब्राइटन कार्नर है।
सूर्यास्त का दृश्य होता है मनोरम
यहाँ पर चीड़ व देवदार के वृक्ष होने के कारण वायु का वेग विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न करता है। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य विशेषकर वर्षा ऋतु में देखने योग्य होता है। कार्तिक के माह में जब आकाश स्वच्छ रहता है, सुनहरे हिमालय का दृश्य देखते ही बनता है। सामने श्यामा देवी का ऊँचा पहाड़ है और बीच की घाटी में शीशे की भाँति चमकती हुई कोसी नदी का मनोरम दृश्य है। यहाँ पर रामकृष्ण मिशन का आश्रम भी है। इस आश्रम में प्रतिवर्ष मायावती को जाने वाले स्वामी विवेकानन्द के अनेक देशी-विदेशी भक्त विश्राम करते हैं।
यहां से अंग्रेजों ने गोरखों के किले पर की थी गोबाबारी
ब्राइटन कार्नर से 2.5 किलोमीटर आगे एक छोटा पहाड़ है जिसे द्योली का डांडा कहते हैं। अल्मोड़ा के समीप घूमने हेतु सिटोली स्थान भी है। यह वही स्थान है। जहाँ से अंग्रेजों ने गोरखों के किले पर गोलाबारी की थी।

पर्वत और प्रमुख नदियां
अल्मोड़ा का पाली पछाऊँ परगना कत्यूर, बारामंडल, फल्दाकोट, कोट व चमोली गढ़वाल के मध्य है। यहाँ के ऊँचे पर्वत जौरासी, द्रोणगिरी, मानिला, नागार्जुन, गुजड़ का डांडा आदि हैं। इस क्षेत्र से बहने वाली प्रमुख नदियाँ रामगंगा, विनौ और गगास हैं। रामगंगा गढ़वाल के पर्वत देवाली खान से निकलकर परगने से बहती है। इसके किनारे गनाई, मांसी भिकियासैण आदि गाँव हैं। बिनौ भी गढ़वाल से निकलकर बूढ़ा केदार के पास रामगंगा में मिलती है। गगास, भाटकोट पर्वत से निकलकर भिकियासैंण में रामगंगा में मिलती है।
प्रमुख मंदिर
इस परगने के प्रमुख मंदिर बूढाकेदार, विभांडेश्वर, चित्रेश्वर, श्रीनाथेश्वर, केदार आदि महादेव हैं। नारायण, नागार्जुन, बदरीनाथ, आदि विष्णु मन्दिर हैं। शीतला, वैष्णवी, मनिलादेवी, भुवनेश्वरी, नैथाणा व अग्नि देवी आदि देवी मंदिर है। शीतला देवी, द्रोणागिरि देवी तथा विभांडेश्वर महादेव का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने किया था। अल्मोड़ा नगर के उत्तर में बाजार के समीप नन्दादेवी का विशाल मंदिर हैं। इस मंदिर में प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है।

इसलिए पड़ा नंदादेवी नाम
मेले का सम्बन्ध कूर्मांचल के चन्द राजाओं के राजघराने से है। कहते हैं किसी चन्द राजा की बहिन के शरीर में एक समय भगवती दुर्गा अवतरित हुई थी, जिसका नाम नन्दा था। दुर्गा सप्तशती में देवी के जिस महात्म्य का वर्णन है, वह नन्दा में प्रत्यक्ष देखने में आया। तभी से वह नन्दा देवी कहलायी जाने लगी। उन्हीं की स्मृति में प्रतिवर्ष यह मेला होता है। अष्टमी के दिन अर्धरात्रि के समय प्रतिमा की स्थापना होती है। नन्दा देवी को प्रतिमा का जोड़ा बनाने का प्रचलन है। प्रतिमा में केवल चेहरा ही रहता है। मेला किसी वर्ष दो दिन तथा किसी वर्ष तीन दिन तक रहता है। स्थापना से लेकर प्रतिमा विसर्जन तक की समस्त विधि कूर्मांचल के राजपरिवार के हाथों से ही सम्पन्न होती है। अल्मोड़ा से दिखायी देने वाली विशाल पर्वत चोटी का नाम नन्दा देवी के नाम पर ही रखा गया है।
जसकोट में भूमि में हैं छोटे छोटे धंसाव
अल्मोड़ा से लगभग आठ किलोमीटर पूर्व की ओर जसकोट नामक स्थान पर भूमि में छोटे-छोटे आकर के गोल या चौकोर धंसाव, पथरीली भूमि पर अथवा बीहड़ चट्टानों पर उकेरे गये हैं। धंसावों में सबसे अधिक प्रचलित ‘ओखला’ गड्ढे हैं, जो कि कप मार्क्स’ के नाम से विख्यात है। इनका सम्बन्ध महाष्म समाधियों से जोड़ा जाता है तथा ये विश्व में कई स्थानों पर देखने को मिले हैं। यद्यपि इनकी तिथि के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। परन्तु पुरातत्व की दृष्टि से इनको प्रागैतिहासिक काल में रखा जा सकता है। यह भी सम्भव है कि नवाष्मयुगीन बुर्जाहोम (कश्मीर) संस्कृति की तरह जसकोट के नाशपति आकार के बड़े धंसावों का प्रयोग आवास हेतु किया जाता रहा होगा। अल्मोड़ा में ऐसे धंसाव छावनी, लक्ष्मेश्वर और नगर से लगे द्योलीडान, चितई और कलमाटिया नामक स्थानों में देखे जा सकते हैं।
ताम्र मानवाकृति मिलने से ताम्र संचय संस्कृति की पुष्टि
अल्मोड़ा में ताम्र मानवाकृति का प्राप्त होना भी पुरातात्विक दृष्टिकोण से आश्चर्यजनक है। 1940 के आस-पास ताम्र मानवाकृति, अल्मोड़ा के बरतन बाजार में देखने को मिली। बनावट और आकार-प्रकार में यह मानवाकृति गंगाघाटी की ताम्रनिधि संस्कृति में पायी जाने वाली ताम्र मानवाकृति सदृश है। इनका भार लगभग पाँच किलोग्राम, ऊँचाई 18 इंच और चौड़ाई पन्द्रह इंच है। 1989 में पिथौरागढ़ जिले में ताम्बे की खान के निकट बनकोट नामक स्थान से आठ ताम्र मानवाकृतियाँ एक साथ प्राप्त हुई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गंगाघाटी की प्राचीनतम ज्ञात धातु-युगीन संस्कृति के निर्माण में उत्तराखण्ड का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

आज भी अल्मोड़ा शहर में टमटा मौहल्ले में ताँबे के आकर्षक बरतन परम्परागत शैली एवं तकनीक से बनाये जाते हैं। इस बात की प्रबल सम्भावना है कि ये शिल्पी ताम्र संचय के रचयिताओं के वंशजों में से एक हों। चूँकि ताम्र संचय संस्कृति द्वितीय सहस्त्राब्दि ईसवी पूर्व में विद्यमान थी, अत: टमटा जाति का इतिहास भी कम से कम इतना प्राचीन माना ही जा सकता है।
दुर्लभ चांदी के सिक्कों से मिली पांच राजाओं की जानकारी
उन्नीसवीं सदी के मध्य में अल्मोड़ा से मिश्रित चाँदी के तीन सिक्के प्राप्त हुए, जिनसे उत्तराखण्ड में दूसरी ईसवी सदी पूर्व से प्रथम ईसवी सदी के तीन शासकों के नाम शिव दत्त, शिव पालित एवं हरदत्त ज्ञात हुए। उन्नीसवीं सदी में ही एक अन्य सिक्का प्राप्त हुआ, जिससे मृगभूति या अमोगभूति राजा का नाम ज्ञात हुआ। इन सिक्कों को
सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय कबीलाई मुद्राओं में विलक्षण एवं दुर्लभ माना जाता है। बीसवीं सदी में इसी प्रकार के 39 सिक्के कत्यूर से प्राप्त हुए, जिनसे गोमित एवं आसेक नामक दो अन्य राजाओं के नाम ज्ञात हुए। इस प्रकार इन प्राप्त सिक्कों से जिन पाँच राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, उन्होंने ईसा पूर्व द्वितीय सदी के अंत से तृतीय ईसवी सदी तक उत्तराखंड में शासन किया। इस तहर के कुछ सिक्के गोविन्द बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में देखने को मिलते हैं।
पढ़ें: जानिए चंपावत जिले के प्रमुख और दर्शनीय स्थल, टनकपुर का क्या था पहले नाम

लेखक का परिचय
लेखक देवकी नंदन पांडे जाने माने इतिहासकार हैं। वह देहरादून में टैगोर कालोनी में रहते हैं। उनकी इतिहास से संबंधित जानकारी की करीब 17 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। मूल रूप से कुमाऊं के निवासी पांडे लंबे समय से देहरादून में रह रहे हैं।
सभी फोटोः साभार सोशल मीडिया