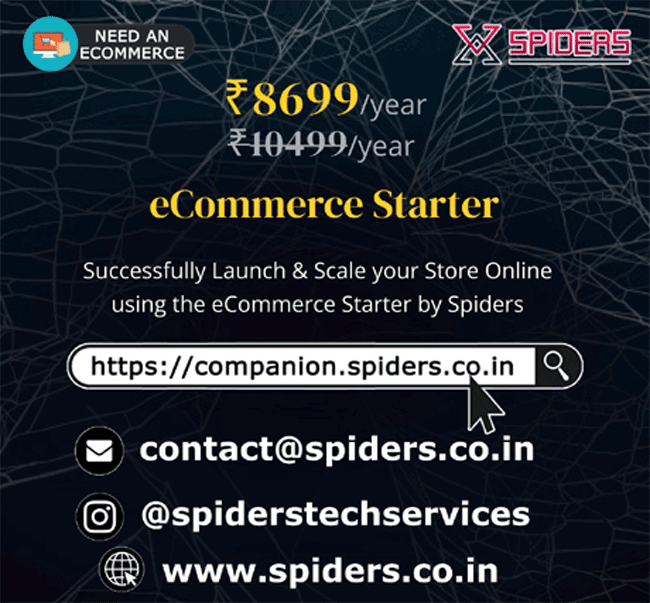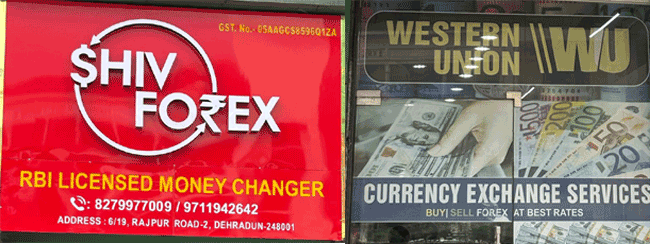पर्यावरण संरक्षण के संदेश का विश्व में बच्चों का एकमात्र त्योहार, आज हो रहा समापन, जानिए वैज्ञानिक व सामाजिक महत्व, धार्मिक कहानियां

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में चैत्र माह के पहले आठ दिनों तक हर घर की देहरी को विभिन्न रंग-बिरंगे फूलों से गुलजार बनाये रखने वाले बच्चों के प्रिय त्योहार फूलदेई पर्व का समापन आज अठ्वाड़ा (आठवें दिन के कार्यक्रम) के साथ हो रहा है। अपने अनोखे रीति-रिवाजों और परम्पराओं के लिए विख्यात उत्तराखंड का यह त्योहार विश्व का एकमात्र त्योहार है जो केवल और केवल बच्चों के द्वारा, बच्चों के लिए समर्पित है। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में प्रकृति के संरक्षण करने का संदेश देने वाले इस अनोखे त्योहार की परम्परायें भी बेहद अनोखी हैं। आइये जानते हैं इस अनोखे त्योहार की कुछ अनोखी परम्पराओं के बारे में।
आठ दिन का है पर्व
चैत्र संक्रांति के दिन से प्रारंभ होने वाले इस त्योहार के पहले आठ दिनों बच्चे अपने – अपने सेवित क्षेत्रों, कस्बे, गांवों की सीमाओं में अवस्थित हर घर की देहरी (दरवाजों) पर रंग-बिरंगे फूल बिखरते हैं। ये फूल घर की देहरी पर इस तरह से रखे (बिखेरे) जाते हैं कि एक भी फूल या फूल की कोई भी पंखुड़ी किसी के भी पाँवों के नीचे न आने पाये। घर के दरवाजों पर फूल बिखेरने की इस परम्परा के पीछे की भावना यह है कि इस घर में पूरे सम्वत (पूरे साल) इसी तरह खुशियां बिखरती रहें। अर्थात इस घर में पूरे वर्ष खुशियां प्रदान करने वाले कार्य सम्पन्न होते रहें। बच्चों द्वारा अपने बड़ों और समाज को शुभकामनाएं देने की यह परम्परा हिन्दू संस्कृति की “वसुधैव कुटुम्बकम” की परम्परा की वाहक और पोषक है।
त्योहार की तैयारी
बच्चे इस त्योहार के आगमन के लिए, कुछ विशेष तैयारी फाल्गुन मास में ही कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला काम होता है रिंगाल से बनी सुन्दर और सजीली टोकरी बनाना। इसे जंगलों से रिंगाल नामक लकड़ी (बाँस की बारीक प्रजाती-जो बहुत लचीली होती है,और जिसे आसानी से मनचाहे आकार में मोड़ा जा सकता है ) लाकर, उसे लम्बाई में बारीक सीखें बनाकर काटा/छीला जाता है। पाठकों की सुविधा के लिए बता दें कि पुराने समय में इसी रिंगाल के छोटे – छोटे टुकड़े बनाकर लिखने के लिए कलम बनाई जाती थी।

सबसे पहले हथकंडी का निर्माण
फिर इससे बच्चों की टोकरियाँ बनाई जाती थी।जिसे स्थानीय भाषा में सजोळी कहा जाता है। कहीं कहीं इसे हथकण्डी भी कहा जाता है।इस टोकरी का आकार(साइज) बच्चे की उम्र और सुविधा के अनुरूप रखा जाता था। (टोकरी बनाने की इस कला के प्रत्येक गांव में कुछ विशेषज्ञ लोगों की सहायता ली जाती थी।) जहां अन्य कामों में प्रयोग के लिए यदि इस टोकरी/हथकण्डी का प्रयोग करना हो तो इसे गाय के गोबर से अन्दर-बाहर लीपा जाता था। परन्तु फूल डालने के लिए इसे बिना गोबर से लीपे ही (कोरा) प्रयोग में लाया जाता है। अब यह टोकरी /हथकण्डी बहुत कम जगहों देखी जाती है। आधुनिकता की चकाचौंध में यह लगभग प्रचलन से बाहर हो गई है, और टोकरी का स्थान वर्तमान में पॉलीथिन या प्लास्टिक मिश्रित थैलियों ने ले लिया है, लेकिन बहुत से गाँवों में अब भी यह टोकरी/हथकण्डी बनाने का काम रिवाज के तौर पर ही सही, पर जिंदा है।
फूलों को चुनना
टोकरी फाल्गुन मासन्त (फाल्गुन माह के अन्तिम दिन) तक तैयार कर ली जाती थी। अब अपनी अपनी इन्ही टोकरियों में बच्चे मासान्ति के दिन (फाल्गुन माह के अन्तिम दिन) गोधूलि बेला में सामूहिक रूप से टोलियाँ बनाकर अपने पर्यावरण का भ्रमण कर, इस मौसम में उगने वाले विभिन्न रंग – बिरंगे फूल चुनकर अपनी – अपनी टोकरियाँ भर लेते हैं। फूलों के रंग उस क्षेत्र के अनुरूप होता है, जहां बच्चे निवास करते हैं । उदाहरणार्थ – हिमालय की तराई में बसे वे गांव जहाँ बुरांस पैदा होता है, उन क्षेत्रों के बच्चे बुरांस के लाल फूलों को जादा चुनते हैं।

फूलों का किया जाता है मिश्रण
अब इसमें उपलब्ध अन्य फूल मिलाये जाते हैं। एक सूर्ख पीले फूल होता है, जो लगभग पूरे उत्तराखंड में पाया जाता है फ्योंली। इसका प्रयोग जरूर हर गांव के बच्चों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अपने अपने क्षेत्रों की उपलब्धता के अनुसार बुरांस, सिन्टाई (सफेद रंग का ट्यूलिप की प्रजाति की तरह का फूल), गोंदा, गुलाब, कनेर, गुड़हल, सिलपाड़ी(बांज-बुराश के जंगलों में आद्र भूमि, जिसमें मिट्टी से जादा पत्थरों की बहुतायत होती है) आदि आदि फूल चुनकर अपनी अपनी टोकरी भर ली जाती है। फूलों के साथ- साथ पंया की पत्तियों (जिसे उत्तराखंड में देव वृक्ष के साथ साथ पितृों का वृक्ष भी कहा जाता है) को भी चुना जाता है। फूलों से भरी इन टोकरियों को घर के बाहर ऐसे स्थानों पर लटका लिया जाता है, जहाँ पर फूलों से भरी ये टोकरियां ताजी हवा और नमी के सम्पर्क में रहें और ताजगी बरकरार रहे।

टोलियों में निकलते हैं बच्चे
अब बच्चे उत्सुकता से अगली सुबह (चैत्र संक्रांति) का इन्तजार करते हैं, ताकि वे अपनी अपनी टोकरियों में भरे फूलों को अपने घर की देहरी में डालते हैं, फिर टोली में इकट्ठा होकर अपने सेवित क्षेत्र के हर घर की देहरियों पर डालते हैं। फूल डालने का यह क्रम भोर होते ही (जिसे स्थानीय भाषा में रतब्यांण या हुरमुर कहा जाता है) प्रारंभ कर दिया जाता है।
कहाँ कितने दिन डाले जाते हैं फूल
कोस-कोस पर बदले पानी, तीन कोस पर बानी” वाली बात इस त्योहार में भी देखने को मिलती है। मध्य नागपुर पट्टी में जहां फूल डालने की परम्परा जहां केवल एक दिन चलती है तो नागपुर की अन्य पट्टियों सहित पूरे जनपद रूद्रप्रयाग में यह प्रक्रिया आठ दिन चलती है। वहीं टिहरी जनपद के अधिकांश क्षेत्रों में फूल डालने की यह प्रक्रिया चैत्र संक्रांति से बैशाख की संक्रांति तक चलती है। टिहरी जिले की चन्द्रबदनी पट्टी के ग्राम रूमधार निवासी सेवानिवृत्त अध्यापक अनसुया प्रसाद उनियाल बताते हैं कि उनके क्षेत्र में नव वर्ष (नया सम्वत) मनाने की यह प्रक्रिया चैत्र संक्रांति से लेकर बैशाख संक्रांति (14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल) तक प्रतिदिन हर घर की देहरी पर फूल डाले जाते हैं।
बैशाखी से होते हैं थौल आयोजित
बैशाखी के दिन से लेकर इसी माह की 19 गते तक न्याय पंचायत स्तर पर, मेलों का आयोजन होता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में “थौळ” कहा जाता है। प्राचीन समय में इन थौळ (मेलों) में एक ओर जहां लोग दूर दूर से आकर एक दूसरे से मेल मिलाप करते थे तो वहीं दूसरी ओर इन मेलों में दूर दूर से आये व्यापारियों से अपनी दैनिक जरूरतों का सामान भी क्रय किया करते हैं। अनुसूया प्रसाद उनियाल आगे बताते हैं कि आज भी लोग यदि किसी से कोई व्यापार करते हैं तो बैशाख के इन थौळों तक रकम अदायगी की कसम ले लेते हैं।
आगे वे बताते हैं कि समय के थपेड़ों और मनोरंजन के आधुनिक तौर तरीकों नें भले ही इन थौळों पर भी अपना प्रभाव डाल लिया हो, लेकिन इन मेलों की आत्मा जिंदा हैं। अभी भी बारगुर, माद्यूं,हिण्डोलाखाल, अंजनीसैंण के थौळ प्रसिद्ध हैं और अपनी पौराणिकता और परम्परा को जीवित रखे हैं,बस एक बात जो बदली है वो ये कि अब इन थौळों में बेला (नर भैंसों) की आपसी लड़ाई नहीं होती। आज से 30-35वर्षों पूर्व इन मेलों का (आकर्षण कहें या विद्रूपता)यह लड़ाई एक प्रमुख कार्य था।

गुड़ तिल चावल की पंरपरा ने लिया नगदी का रूप
उत्तराखंड के बहुत से हिस्सों में बाल पर्व का यह फूलदेई त्योहार पहले ही दिन मनाया जाता है। बच्चे जैसे ही फूलदेई के गीत गाते सुनाई देते हैं, परिवार की मुखिया (घर की वरिष्ठ महिला बच्चों के लिए चावल, गुड़-तिल लेकर तैयार रहती थी। जैसे ही बच्चे घर की देहरी पर फूल डालते, वैसे ही घर की मुखिया बच्चों के प्रमुख को गुड़-तिल का भेंट करती और प्रत्येक बच्चे को सामर्थ्यानुसार चावल भेंट करती। बच्चों का मुखिया हाथ में पिंठाईं का थाल लिए रहता है, जो मुखिया का तिलक करता है। परम्परागत रूप से टोली के बच्चों को एक – एक मुट्ठी भर चावल मिलता है। जिसके लिए बच्चे अपने कन्धों पर थैला भी लटकाये रखते। अगर एक ही परिवार के एक से ज्यादा बच्चे टीम में शामिल होते तो परिवार के सबसे बड़े बच्चे के थैले में ही सबके बदले के चावल दे दिये जाते। अब आधुनिक होते समाज में गुड़ तिल चावल की परम्परा ने नगदी का रूप ले लिया है, परन्तु फिर भी कुछ गांवों में ये परम्परा निर्बाध रूप से गतिमान है।
डोली को भी नचाते हैं बच्चे
जहाँ फूल डालने की ये परम्परा आठ दिन चलती है, वहां पिंठाईं का थाल लिए हुए मुखिया की थाली में उस परिवार की मुखिया अपनी सामर्थ्यानुसार कुछ नकदी या सिक्के रख देती। यहां विशेषता की बात यह है कि इस टोली में चावल सामूहिक रूप से एक ही बच्चे को दिए जाते हैं। दो बच्चे अपने कन्धों पर घोघा डोली लिए रहते हैं, वे डोली को नचाते हैं, टोली के अन्य बच्चे फुलारी गीत गाते हुए फूल डालते बढ़ते रहते हैं।

क्या है घोघा
जिन क्षेत्रों में यह बाल पर्व आठ दिनों तक चलता है, वहाँ बच्चों की इस फूल डालने वाली प्रभात फेरी में दो बच्चों के कन्धों पर एक देव डोली सदृश डोली होती है। जहां देव डोली में किसी न किसी देवता की प्रतिमा विराजित होती है, वहीं घोघा डोली में कोई प्रतिमा नहीं होती। इसमें डोली के मध्य में लगी एक लकड़ी के सहारे कुछ रंग – बिरंगी चुन्निया /कपड़े बांध कर लटका दिए जाते हैं। जिन्हें साड़ा या साड़े कहा जाता है। इस डोली को ही घोघा देवता कहा जाता है। अब तक के शोध में कहीं यह कोई प्रमाण हीं मिला कि घोघा पुल्लिंग देवता है या स्त्रीलिंग (देवी)। लेकिन शोध के दौरान बहुत सी जनश्रुतियां और किंवदन्तियाँ सामने आई हैं, जिन्हें पाठकों के समक्ष रखा जा रहा है-
ये है कहानी
बहुत से लोग घोघा को श्रीकृष्ण के कालिय नाग दमन के साथ जोड़कर देखते हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि घोघा हिन्दुओं के देवता भगवान श्रीकृष्ण का रूप है। वर्ष 1995 में इस विषय पर जब मैन शोध दिया तो बातचीत में ऊखीमठ ब्लॉक के ग्राम स्याँसू निवासी थेपड़ सिंह ने बताया कि- हिन्दू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार गायों को चराते समय ग्वाल-बालों के संग खेलते समय जब गेंद यमुना में गिर गई थी। जब कृष्ण गेंद लेने यमुना में कूद पढ़ते हैं तो वहां कालिया नाग के साथ युद्ध करके परास्त करने में देर हो जाती है। ग्वाल-बाल उन्हें यमुना में डूब कर मृत समझ लेते हैं, परन्तु कुछ देर बाद जब श्री कृष्ण वापस लौटते हैं। ग्वाल-बाल उन्हें जीवित पाकर खुशी से कन्धों पर उठाकर गोकुल का चक्कर लगाते हैं। श्रीकृष्ण के इसी रूप को अब घोघा के रूप में कन्धों पर उठाकर घुमाया जाता है।
ये भी है मान्यता
कुछ लोग गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल की रक्षा करने की खुशी और इन्द्र के घमंड को चूर करने के लिए घोघा को श्री कृष्ण के प्रतीक रूप में भी बताते हैं। फूल डालने की इस परम्परा के बारे में कुछ लोगों की मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर तपस्यारत शंकर को जगाने के लिए माता पार्वती ने कैलाश के नजदीक बर्फ रहित भूमि पर अपने तपोबल से नाना प्रकार के सुगन्धित पुष्प खिला (पैदा) किए। उन पुष्पों को एकत्र कर शंकर के आसन के आस पास बिखेर दिया। पुष्पों की सुगंध से शंकर को तपस्या से बाहर लाने की खुशी में माता पार्वती के भक्तों से कालांतर में यह पर्व के रूप में प्रचलित हो गया। ये तथ्य वास्तविकता के कितने नजदीक हैं इसके लिए अभी तक कोई लिखित या ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका है। जिसपर विभिन्न लोगों और संस्थाओं द्वारा शोध कार्य करने की जानकारी मिली है।
क्या है अठ्वाड़ा मनाने का कारण
हमारी सनातन पद्धति का यदि आप बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना विश्लेषण करें तो आप पायेंगे कि इसके हर नियम और हर जीवन पद्धति सूत्र के पीछे सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव निहित है। भारतीय जीवन पद्धति का एक भी सूत्र ऐसा नहीं है, जिसमें केवल स्व का हित निहित हो। इसके हर सूत्र में सर्वे भवन्तु सुखिनःकी मूल भावना निहित है। अतः यह अठ्वाड़ा पर्व एक तरह से प्रकृति से लगातार आठ दिनों तक फूल बीनते हुए उसे हुई क्षति की क्षमा प्रार्थना का पर्व भी है।
रूद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ ब्लॉक की ग्राम पंचायत जाल मल्ला के प्रधान त्रिलोक सिंह रावत का कहना है कि अठ्वाड़ा प्रकृति को आठ दिनों तक फूल चुनने के कारण हुए दोहन की क्षमा प्रार्थना के रूप में भी लिया जा सकता है। लेखक का मानना भी है कि अठ्वाड़ा प्रकृति से विभिन्न प्रकार के फूलों को चुनने के कारण हुए दोहन के लिए क्षमा प्रार्थना है, क्योंकि इस दिन फुलारी(फूल डालने वाले बच्चे) वन में जाकर वन देवता की पूजा – अर्चना करते हैं। जिसका अप्रत्यक्ष अर्थ यही है कि “हे वन देवता हमारे दोहन के लिए हमें इस बात के लिए क्षमा करना कि हमने फूलों के रूप में आपका दोहन किया है। अट्वाडे के दिन बच्चे आठ दिनों तक प्राप्त सामग्री व धन से प्राप्त भोज्य पदार्थ क्रय कर सर्व प्रथम प्रकृति (वन देवता) को ही भोग लगाते हैं। आइए जानते हैं अब इस त्यौहार और बाल पर्व के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कारण।
मनोवैज्ञानिक कारण
यदि आप तनिक पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि फरवरी माह तक मौसम में सर्दी होने के कारण प्रात: बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। विशेषकर बच्चे इस मौसम में (मार्च आने पर भी) बिस्तर से आदतन उठ नहीं पाते। धार्मिक से जादा इसे मनोवैज्ञानिक कहें तो जादा उचित होगा। बच्चों को यदि यह कहा जाता है कि तुम्हें सुबह फूल डालने जाना है तो बच्चे स्वाभाविक रूप से जल्दी उठ जाते हैं, जो उनके बढ़ते स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है।
इस त्योहार में फूल बीनने के लिए बच्चे अपने आस पास के पर्यावरण में जाते/घूमते हैं। जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार के फूलों, वनस्पतियों का अवलोकन करने का मौका मिलता है। अतः उनमें जल्दी उठने, समूह में काम करने, आपसी संवाद स्थापित करने, फूलों और वनस्पति की जानकारी का उन्हें मौका मिलता है।
सामाजिक कारण
बच्चों को अपने पास-पड़ोस के बच्चों के साथ घुलने मिलने का मौका मिलता है। ऐसे माहौल में (फूलदेई के अवसर पर) वे एक दूसरे से के निकट आते हैं। जिससे समाज में आपसी सामंजस्य और सौहार्द में वृद्धि होती है। साथ ही उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास भी होता है।

स्वास्थ्य संबंधी कारण
चैत्र में बसंत का आगमन होने से प्रकृति में नाना प्रकार के फूलों के खिलने का क्रम प्रारंभ हो जाता है। जिस कारण इस मौसम में वातावरण में नाना प्रकार के औषधीय पादपों की सुगन्ध से वातावरण सुगन्धित हुआ रहता है। अतः ऐसे माहौल में प्रातः बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए सैर करना संजीवनी पाने जैसा होता है। चैत्र याने मार्च आते आते मौसम में भयंकर सर्दी की ठिठुरन काफी कम हो जाती है। ऐसे मौसम में भयंकर सर्दी के कारण अपनी प्रात:सैर करने की आदत को पुनः प्रारंभ किया जा सकता है। जो शारीरिक दृष्टि से मजबूत होने के लिए भी बेहतर है। अतः फूलदेई याने चैत्र का महीना सर्वाधिक उपयुक्त है।
वैज्ञानिक कारण
सम्पूर्ण उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भौगोलिक बनाबट के कारण जहाँ सर्दियों में (नवम्बर से फरवरी तक) यहाँ का औसत तापमान जहाँ 1से 6 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं मार्च आते आते यह औसत तापमान 6 से 13 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सुखनुमा माहौल में सैर करना डाक्टरी नजरिये से शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता।
बच्चों को अपने आस पास के वातावरण /परिवेश में फूल बीनने के दौरान उनका परिचय विभिन्न फूलों, लताओं, बेलों से हो जाता है, जिससे उनकी अवलोकन की क्षमता के साथ – साथ विश्लेषण की क्षमता का भी विकास होता है। बच्चों में फूल डालने के लिए जाने के कारण सुबह उठने और सैर करने की आदत स्वत: ही बन जाती है, साथ ही समूह में घुलने – मिलने, साथ काम करने की प्रवृत्ति भी विकसित हो जाती है। जो बातें किताबें महीनों में नहीं सिखा पाती उन्हें बच्चे बड़ी उमंग, उत्साह और आनंद के साथ चैत्र मास के इस हफ्ते में ही सीख जाते हैं।
अतः वैज्ञानिक अनुसंधान के दृष्टिकोण से भी देखें तो फूलदेई महोत्सव के इस बाल पर्व को बच्चों के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास के लिए बहुत ही उपयुक्त, उपयोगी और महत्वपूर्ण कहा जा सकता है।
आज अठवाड़े को समापन
इस पर्व का आज आठवां दिन है। अधिकांश स्थानों में अठवाड़े के दिन इसका समापन हो जाएगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पश्चिम का अंधानुकरण न करते हुए, अपनी विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धति की जीवन शैली को महत्व देते हुए उसे अपनाने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें, और साथ ही मंच और मौके भी उपलब्ध करायें। मैं इस अपील के साथ ही माननीय उत्तराखंड सरकार से निवेदन करता हूँ कि वे बच्चों की बाल भावनाओं का सम्मान करते हुए इस फूलदेई महोत्सव पर्व को राज्य पर्व घोषित करते हुए फूलदेई के आठवें दिन (अठ्वाड़े को) सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हुए इसे राज्य बाल पर्व भी घोषित करे।

लेखक का परिचय
नाम- हेमंत चौकियाल
निवासी-ग्राम धारकोट, पोस्ट चोपड़ा, ब्लॉक अगस्त्यमुनि जिला रूद्रप्रयाग उत्तराखंड।
शिक्षक-राजकरीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय डाँगी गुनाऊँ, अगस्त्यमुनि जिला रूद्रप्रयाग उत्तराखंड।
mail-hemant.chaukiyal@gmail.com
लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
वाट्सएप नंबर-9412055165
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।