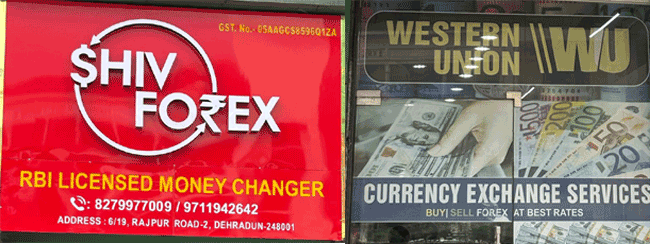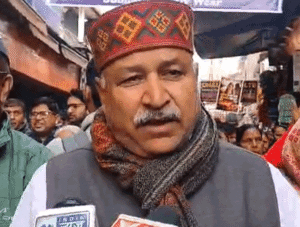देहरादून में डाकपत्थर के आसपास का क्षेत्र अपने मे समेटे हुए है एक इतिहास, आप भी जानिए
देहरादून के आंचल में बसा और जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर हिमाचल व उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ परियोजना क्षेत्र डाकपत्थर है। डाकपत्थर सहित आसपास का क्षेत्र अपने में एक इतिहास समेटे हुए है। यहां पर्यटक आते हैं और ऐतिहासिक अवशेष देखकर हैरान हो जाते हैं। यहां बताते हैं ऐसे ही स्थलों के बारे में।

डाकपत्थर कई महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं की मुख्य कार्यस्थली होने के कारण पर्यटकों में दर्शनीय रहा है। साथ ही यह क्षेत्र अपनी अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यता एवं शिवालिक पर्वत श्रेणियों से घिरे अपने नैसर्गिक परिवेश के कारण भी पर्यटकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है।
विद्युत परियोजना क्षेत्र में महत्वपूर्ण
किशाऊ बांध परियोजना, लखवाड़-व्यासी बांध परियोजना और विशेष भूगर्भ छिवरऊ पावर हाउस जैसी राष्ट्रीय धरोहरों को अपने आंचल में समेटे हुए यह परियोजना क्षेत्र तकनीकी कारणों से अति महत्वपूर्ण है। सिंचाई विभाग यमुना जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत यहां पर यमुना और टौंस नदी के संगम पर करोड़ों की लागत से एक बैराज निर्मित है। इसका शिलान्यास देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था। यहां से यमुना और टौंस नदी का पानी शक्ति नहर के जरिये ढकरानी विद्युत पावर हाउस के लिये लाया जाता है। ढकरानी से 3 किलोमीटर आगे ढालीपुर पावर स्टेशन को पानी भी इसी शक्ति नहर से पहुंचाया जाता है।

डाकपत्थर से कुछ ही दूरी पर स्थित टौंस नदी के किनारे भारतीय इंजीनियरों व वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी तकनीक से 240 मेगावाट क्षमता का एक भूगर्भ पावर हाउस बनाया गया है। डाकपत्थर से आगे कोटी में भी एक बांध निर्मित है। यहां से नदी का पानी 2.5 किलोमीटर लम्बी सुरंग द्वारा छिबरऊ स्थित अंडरग्राउण्ड पावर हाउस तक पहुंचाया जाता है। यह भूगर्मीय पावर हाउस राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है।
पर्यटकों के लिए आकर्षण
पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गढ़वाल मण्डल विकास निगम ने यहाँ पर पर्यटक आवास गृह का निर्माण कराया है। यहाँ से डाकपत्थर बैराज का रात्रि दृश्य विद्युत लैम्पों की जगमगाहट में दर्शनीय है।
अशोक का शिलालेख
देहरादून के पश्चिम छोर में 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कालसी, अशोक शिलालेख के कारण इतिहास में अपना एक विशेष स्थान बनाये हुए है। प्राचीन भारत में इतिहास के तिथि क्रमों को श्रृंखलाबद्ध जोड़ने का कोई प्रयत्न किसी युग में नहीं किया गया। इस कारण आज हमारे देश का इतिहास कड़ी-कड़ी रूप में इधर-उधर बिखरा पड़ा है। उसे एक सूत्र में बांधने में इतिहासवेत्ताओं को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। संयोगवश भारतीय इतिहास और संस्कृति के रक्षक सम्राट अशोक ने अपने काल का इतिहास आत्मचरित के रूप में स्तम्भों व चट्टानों पर खुदवा दिया था।
अशोक के शिलालेख इस समय भारत के कोने-कोने में स्थापित हैं। इनके सुदूर स्थानों में पाये जाने से यह भी प्रमाणित होता है कि अशोक की राज्य सीमा कहां तक थी। कालसी में चट्टान पर लिखा गया ऐसा ही एक शिलालेख सन् 1860 में श्री फारेस्ट द्वारा खोज निकाला गया। उस समय यह मिट्टी आदि से इस प्रकार ढका हुआ था कि उत्कीर्ण लेख स्पष्ट नहीं था।

यह शिलालेख अशोक के चौदह लेखों का पाठान्तर है। यह लेख राज्याभिषेक के पश्चात चौदहवें वर्ष में तथा ईसा से 250 वर्ष पूर्व अंकित किया गया था। यह चौदह शिलालेख प्रायः परिपूर्ण अवस्था में अन्य स्थानों पर भी प्राप्त होते हैं। कालसी शिलालेख का अधिकांश भाग प्रस्तर के दक्षिण कक्ष में मिलता है, किन्तु शब्दों के बड़े होने तथा नीचे की ओर बढ़ने के कारण निर्धारित स्थान सम्पूर्ण लेख के लिए अपर्याप्त प्रतीत हुआ, अतएव उसको शिला के पश्चिम कक्ष में पूर्ण किया गया। शिला के पूर्वी कक्ष में एक हाथी का चित्र अंकित है तथा अंगों के बीच में गजतम’ शब्द भी अंकित हैं।
बौद्धकला में हाथी का विशेष महत्व
बौद्धकला में हाथी को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। कथा है कि भगवान बुद्ध तुषित स्वर्ग से आकर माता के गर्भ में एक हाथी के रूप में प्रविष्ट हुए थे। यह लेख प्राचीन ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है जो कि बायें से दायें लिखी जाती थी। यही लिपि आधुनिक देवनागरी तथा अन्य भारतीय लिपियों की जन्मदात्री है। कालसी के शिलालेख में देश के अन्य भागों से प्राप्त शिलालेखों की तरह अशोक ने ‘देवानांप्रिय’ शब्द प्रयुक्त किया है। यह पद सर्वथा नवीन नहीं है।

‘मुद्राराक्षस’ नाटक में भी एक स्थल पर सम्राट चन्द्रगुप्त को ‘देवानांप्रिय’ कहकर संबोधित किया गया है। शिला स्तम्भ अशोक के ही बनवाये हुए हैं, इसका प्रमाण मास्को के एक शिलालेख से प्राप्त हुआ है। क्योंकि उसमें देवानांप्रिय के साथ अशोक लिखा हुआ है। इन शिलालेखों के आधार पर स्पष्ट होता है कि अशोक गाँवों की भारतीय जनता के लिए ‘जानपद जन’ नामक सम्मानित शब्द का प्रयोग करते थे और उनके हृदय में देश की जनता के लिए अगाध स्नेह था।
जनता से सम्पर्क साधने के लिए उन्होंने कई नये उपायों का सहारा लिया। अभी उनको सिंहासन पर बैठे दस ही वर्ष हुए थे, कि सामंतों की विहार यात्राओं को रद्द करके लोक जीवन से स्वयं परिचित होने के लिए उन्होंने एक नये प्रकार के दौरे का विधान किया, जिसका नाम ‘धर्मयात्रा’ रखा गया। इसका उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित था। ‘जानपदसा च जनसा दसने धर्मनुसधि च धम पलिपुछा च’। कालसी में स्थित शिलालेख पर ये शब्द खुदे हुए हैं। धर्म के लिए होने वाले इन दौरों का उद्देश्य था – जनपद जन का दर्शन,उनको धर्म की शिक्षा देना व उनके साथ धर्म विषयक पूछताछ करना।

अश्वमेध यज्ञ एवं प्राप्त अवशेष
देहरादून जिले के पश्चिम में लगभग पचास किलोमीटर की दूरी पर स्थित जगत ग्राम में चार अश्वमेध यज्ञ सम्पूर्ण होने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये अश्वमेध यज्ञ राजा शीलवर्मन् द्वारा तीसरी शताब्दी में सम्पन्न कराये गये। राजा ने कालसी के समीप जगत ग्राम में गरूड़ाकार वेदिका बनाकर ईटों पर निम्न अभिलेख अंकित कराये थे-
(अ) सिद्धम् ! युगेश्वरस्याश्वमेधे युगेशैलमहीपते
इष्टका वाषगण्यस्य नृपतेश्शीलवर्मण।
(आ) नृपते बर्षिगण्यस्य पोण-षष्ठस्य श्रीमत
चतुर्थस्याश्वमेधस्य चित्यो ! यं शीलवर्मण ।
अर्थात् शीलवर्मन् वार्षगण्यगोत्र में उत्पन्न हुआ था। उसके छटे पूर्व पुरूष का नाम पोण था। उसने चार अश्वमेध किये थे। उन दिनों उसके शासित प्रदेश का नाम या उसकी राजधानी का नाम युगशैल था। वर्तमान में इस गोत्र के वंशज उत्तराखंड में नहीं मिलते। महाभारत के अनुसार वार्षगण्य एक प्राचीन ऋषि थे, जो सांख्य के प्राचीन आचार्य माने जाते थे। उनका जीवन काल दूसरी शती ईसवी का हो सकता है। उनकी छटी पीढ़ी में उत्पन्न शीलवर्मन् का काल तीसरी शती ईसवी में माना जा सकता है।

लाखामंडल में मिलते हैं राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख
शीलवर्मन् के इष्टकालेख की तिथि लिपि के आधार पर तीसरी शती ईसवी निश्चित की गयी है। इसी शती के अंतिम वर्षों के आस-पास यमुना घाटी में सेनवर्मन् ने यदुवंश के राज्य की स्थापना की। जिसके बारह नरेशों के नाम लाखामण्डल में प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख से मिलते हैं।
शीलवर्मन् के इष्टकालेख में उसके शासित प्रदेश का नाम युग और युगशैलम् ही आया है। कुछ
पुरातत्वविदों का मानना है कि युगशैल या युग नामक पहाड़ी प्रदेश सम्भवत: अम्बाला से लेकर यमुना नदी के पार तक फैला था। जिस स्थान पर शीलवर्मन् ने अश्वमेध की यज्ञवेदी का निर्माण किया, वह स्थान जगत ग्राम यमुना के पूर्वी तट पर स्थित है। अत: शीलवर्मन् का राज्य यमुनातट से पूर्व की ओर विस्तृत क्षेत्र में फैला रहा होगा। युगशैलमही का अर्थ दो पर्वतों से घिरी भूमि भी हो सकती है। उपगिरि या शिवालिक श्रेणी से लेकर अन्तर्गिरि या लघुहिमालय तक अथवा वहिगिरि या महाहिमालय तक के प्रदेश को युगशैलमही कह सकते हैं।
चार अश्वमेध, करने वाले नरेश का अधिकार संभवतः सारे कुलिन्द जनपद पर रहा होगा। जगतग्राम, कालसी के ठीक सामने यमुना के बायें तट पर है। कालसी या कालकूट अति प्राचीनकाल से कुलिन्द जनपद का मुख्यालय, राजधानी या प्रमुखनगर रह चुका है।
जगतग्राम उत्खनन में प्राप्त यज्ञवेदिका पक्की ईटों से बनी है। आकार में यह यज्ञवेदिका उड़ते हुए गरूड़ पक्षी के समान है। इसकी लम्बाई 24 तथा चौडाई 18 मीटर है। इसका मुख पूर्व दिशा की ओर है व दो चौड़े पंख उत्तर-दक्षिण में हैं। इसके निर्माण में विभिन्न आकार की ईटों को प्रयोग में लाया गया है, जिनका माप 80x50x11 सेंटीमीटर से लेकर 50x50x11 सेंटीमीटर है। वेदिका के बीचों बीच एक 120 x 120 सेंटीमीटर का यज्ञ कुण्ड भी प्राप्त हुआ है। जिसकी गहराई 2.60 मीटर है। इसमें जली हुई लकड़ी के टुकड़े व राख प्राप्त हुई है।
समुद्रगुप्त से पूर्व के माने गए
अश्वमेधकर्ता शीलवर्मन् की राज्यावधि सम्राट समुद्रगुप्त से पूर्व की है, क्योंकि प्रचण्ड पराक्रमी समुद्रगुप्त के राज्यकाल में उसका अदना सा पड़ोसी अश्वमेध की कल्पना भी न कर सकता था। शीलवर्मन् का इष्टकालेख शुद्ध संस्कृत में छन्दोबद्ध है। लिपि के आधार पर उसे तीसरी शती ईसवी में माना जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि शीलवर्मन् के अश्वमेध की तिथि समुद्रगुप्त के राज्यारोहण की तिथि से पूर्व की ही हो सकती है।
शुंगकाल में गरूड़ाकृति को विशेष पावनता मिल चुकी थी अत: शीलवर्मन् ने भी यज्ञ के लिए गरूड़ाकार वेदिका बनवाई थी। शीलवर्मन् के राज्याकाल में स्त्रुघ्न, कालकूट, बेहट, जगतग्राम वीरभद्र, मायापुर, पाण्डुवाला और गोविषाण आदि व्यापार के केन्द्र थे।

लेखक का परिचय
लेखक देवकी नंदन पांडे जाने माने इतिहासकार हैं। वह देहरादून में टैगोर कालोनी में रहते हैं। उनकी इतिहास से संबंधित जानकारी की करीब 17 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। मूल रूप से कुमाऊं के निवासी पांडे लंबे समय से देहरादून में रह रहे हैं।