महाभारत के विलेन दुर्योधन और कर्ण की यहां होती है पूजा, दुर्योधन के आदेश पर 1986 में लूटी गई थी भेड़, जानिए रोचक कथाएं
क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत काल में जिस दुर्योधन को युद्ध का मुख्य कारण माना गया। जो उस समय का मुख्य विलेन रहा हो, वो भी पूजनीय है। उसका भी मंदिर है। साथ ही दानवीर कर्ण का भी मंदिर उत्तराखंड की धरती पर है। दुर्योधन का ही असर है कि इस कलयुग में भी उसका आदेश चलता है। दुर्योधन के आदेश पर हिमाचल और उत्तराखंड के ग्रामीणों के बीच विवाद भी हो चुका है। ग्रामीणों की भेड़ भी लूटी जा चुकी हैं। उत्तरकाशी के मंदिरों की ऐसी ही रोचक कहानी यहां आपको बताने जा रहे हैं।
दुर्योधन का पूजा स्थल
उत्तरकाशी जिले में नैटवाड़ से हर-की-दून और जखोल क्षेत्र तक पंचगाई क्षेत्र है। इस क्षेत्र को पंचगाई, अडोर और बड़ासू पट्टियों में बाँटा गया है, जिसमें 21 गाँव है। इन सभी गाँवों में दुर्योधन को ही मुख्य देवता माना और पूजा जाता है। दुर्योधन की आज्ञा पर ही यहाँ का समस्त कार्य संचालित किए जाते है। सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी भी यहाँ की रीति-रिवाजों के समक्ष स्वयं को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं।
दुर्योधन का मानना होता है आदेश
कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर दुर्योधन की आत्मा आती है, वह व्यक्ति नाचकर कुछ भी आदेश गाँववासियों को देता है। ऐसे आदेशों का पालन करने के लिए क्षेत्रवासी भी वैसा ही करते हैं। सन 1986 में दुर्योधन ने आदेश दिया कि हिमाचल के सीमावर्ती गाँववालों ने इस क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। अत: उनकी सभी भेड़ों को लूटकर ले आओ। परिणामस्वरूप जखोल (दुर्योधन का मुख्य स्थान) में पंचायत हुई और रात में सभी गाँव के लोग एकत्र हुए। इसके बाद हिमाचल क्षेत्र के गाँवों की तीन सौ से अधिक भेड़ों को अपने क्षेत्र में ले आये।
दो सरकारों को करना पड़ा हस्तक्षेप, पर माना दुर्योधन का आदेश
विवाद यहाँ तक पहुँचा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बावजूद इस क्षेत्र के लोग नहीं माने। अन्ततः दुर्योधन के पास फरियाद की गई। उसने आदेश दिया कि हिमाचल के गाँव वाले दण्ड दें, तभी उनकी भेड़ें वापिस की जायें। दुर्योधन का आदेश हिमाचल के गाँववालों को सुनाया गया। परिणामत: शासन की बात को न मानकर दुर्योधन की बात को प्रमुखता दी गई। दंड प्राप्त होने पर हिमाचल वालों को भेड़ें वापिस की गई।
कर्ण देवता मंदिर
उत्तरकाशी जिले के नेतवार गाँव से लगभग डेढ़ मील दूर सारनौल गांव में स्थित एक प्राचीन एवं लोकप्रिय मंदिर है। यह मंदिर महाभारत के समय से संबंधित है। यह मंदिर कर्ण को समर्पित है, जिसे पांडवों में सबसे बड़ा भाई माना जाता है। कर्ण देवता मंदिर को शक्ति और शांति का प्रतीक माना जाता है। कर्ण देवता मंदिर के निकट तमस या टोंस नदी है। इस नदी के बारे में यह मान्यता है कि भुब्रूवाहन के आंसुओं के कारण ही यह नदी बनी थी।
कर्ण की होती है पूजा
कर्ण देवता मंदिर के अलावा उत्तराखंड के सीमांत जनपद मोरी ब्लॉक के 24 गांव ऐसे हैं, जहां लोग दानवीर कर्ण की पूजा करते हैं। इस क्षेत्र के लोग कर्ण देवता को अपना ‘कुल देवता’ और ‘ईष्ट देवता’ मानते हैं। कर्ण देवता महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र हैं। लोग इस मंदिर में भगवान कर्ण और अन्य देवी-देवताओं की पूजा करते हैं।
नहीं दी जाती पशु बलि, करते हैं दान
इस क्षेत्र के लोगों की कर्ण के प्रति इतनी आस्था है कि गाँव में अधिकतर मंदिर कर्ण और कर्ण के साथी द्वारपालों व कर्ण की गुरुमाता के हैं। अपने दान के कारण प्रसिद्ध कर्ण देवता मंदिर में भी लोग श्रद्धापूर्वक दानकर्म करते है। मंदिर परिसर में लोग धार्मिक कार्यो, अनुष्ठान और पुण्य दान करने आते हैं। कर्ण देवता की अच्छी आदतों को सम्मान देने के लिए इस क्षेत्र के गाँव में दहेज प्रथा को बंद कर दिया है। मंदिर परिसर में किसी भी धार्मिक कार्यों या पूजा विधि में किसी भी जानवर की बलि भी नहीं दी जाती है।

मंदिर बनाने की कथा
सारनौल (कर्ण देवता मंदिर) और सौर ( दुर्योधन मंदिर) नाम के दो गांव की भूमि महाभारत काल के महान योद्धा भुब्रूवाहन की धरती मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि राजा भुब्रूवाहन कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध में कौरव सेना का हिस्सा बनना चाहते थे, किंतु उसकी शक्ति से भली भांति परिचित भगवान कृष्ण ने बड़ी ही चालाकी से भुब्रूवाहन का सिर उसके धड़ से अलग करके उन्हें युद्ध से दूर कर दिया। जब उसने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की तो उसकी योग्यता के चलते ये अधिकार देते हुए कृष्ण जी ने उसके सिर को एक पेड़ पर टांग दिया और उसने वहीं से महाभारत का पूरा युद्ध देखा।
इसलिए नहीं पीते तमसा का पानी
कहते हैं कि वो कौरवों की हार देखकर बहुत रोता था और दोनों गांवों के समीप जो नदी है, वो भुब्रूवाहन के आंसुओं के कारण ही बनी थी। इसे तमस या टोंस नदी के नाम से जाना जाता है। इसी धारणा के चलते इस नदी का पानी पीने योग्य नहीं माना जाता। उत्तरकाशी के लोकगीतों में भब्रूवाहन के साथ दुर्योधन और कर्ण की प्रशंसा की जाती है और उन्हें देवताओं के समान पूजा जाता है। इसी कारण इस क्षेत्र में मंदिर का निर्माण किया गया।
विश्वनाथ मंदिर
यह मंदिर नगर के मध्य स्थित है। वास्तुकला के दृष्टिकोण से यह सर्वोच्च है। मंदिर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका जीर्णोद्धार कई बार हो चुका है। पत्थर के सुन्दर टुकड़ों और मूर्तियों से
इसकी प्राचीनता का पता सहज ही लग जाता है। मंदिर के आँगन में ही सामने एक शक्ति स्तम्भ है।
जिसे त्रिशूल, ध्वजस्तम्भ या जयस्तम्भ भी कह सकते हैं। इसके नीचे का भाग, लगभग तीन
फुट लम्बाई में ताँबे के शिखर से प्रतिबद्ध किया हुआ है, स्थानीय जनों का विश्वास है कि इस
तरह के सात शिखर भूमि के भीतर हैं। ऊपरी भाग जो कि 17 फीट लम्बाई में है, पंच धातु का है। ऊपरी कोने में, जहाँ त्रिशूल और फरसा बना है, तीन फीट लम्बाई में लोहे का दिखता है। इसकी कुल ऊँचाई पृथ्वी तल से 21 फीट है। दो फीट की मोटाई से अष्टकोण बना है।
लिखे हुए हैं लेख
इसके दो पहलुओं पर तीन पंक्तियों का एक लेख, दो फीट लम्बा खुदा हुआ है। इसमें पहली पंक्ति कुछ छोटे अक्षरों से लिखी गयी है, जो शार्दूलविक्रीड़ित छन्द का एक श्लोक है। दूसरी में बड़े अक्षरों से उसी छन्द का एक अन्य श्लोक, तीसरी में बहुत बड़े बड़े अक्षरों से एक नगधरा’ लिखी गयी है। पूरा लेख शुद्ध संस्कृत में साफ और सुन्दर है। लेख का अर्थ इस प्रकार है- “प्रज्ञानुरागी गणेश्वर नामक राजा अत्यन्त उन्नत श्री विश्वनाथ का मन्दिर बनवाकर, मंत्रियों सहित अपनी राज्यलक्ष्मी को अणु समझकर और उसे प्रियजनों के वंश में देकर इन्द्र की मित्रता की याद में उत्सुक हो, सुमेरू मंदिर (स्वर्ग या कैलाश) चला गया।” दूसरे श्लोक में “हिमवच्छृगोच्छृत” है, इससे यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता कि उसने सम्पूर्ण मंदिर को बनवाया या शिखरों का ही संस्कार करवाया था।

स्तंभ लेख की लिपी है प्राचीन
“वनजधिप” शब्द से वह किसी वनाच्छादित प्रदेश का राजा मालूम पड़ता था। “शुक्रसृहत” शब्द, राजा को अत्यन्त बलशाली सिद्ध करता है। राजा गणेश्वर के बाद उसके पुत्र श्रीगुह के हाथ में राज्य आया, जो अत्यन्त बलशाली, विशाल नेत्र और दृढ़ वक्षस्थल बाला था। उसने सौन्दर्य में मन्मथ को, दान में कुबेर को, नीति या शास्त्र में वेद व्यास को जीत लिया था। वह धार्मिकों का अगुआ और
बड़ा उदार था। उसने ही भगवान के सामने एक शक्तिस्तम्भ की स्थापना की थी। उसे देखते ही शत्रु लोग डर जाते थे, क्योंकि वह प्रतापी और सुंदर गुण वाला था। जब तक भगवान सूर्य अपनी तरूण किरणों से गाढ़ान्धकार को नष्ट करके नक्षत्रों की चित्र चर्चा को मिटाकर गगन फलक में अपने बिम्बरूपी तिलक को लगाते रहें, तब तक प्रतापी राजा गृह की यह कीर्ति सुस्थिर रहे। लिपि के विचार से यह कहा जा सकता है कि यह राजा विक्रमी सम्वत् की पांचवीं या छठी शताब्दी में हुआ होगा। इस स्तम्भ लेख की लिपि गुप्तकाल लिपि के आसपास की है।
परशुराम मंदिर
अष्टधातु निमित परशुराम की मूर्ति तथा जीर्ण अवस्था में पड़ा यह मंदिर उस युग की याद दिलाता है जब परशुराम ने इस स्थान पर तपस्या कर शिव के दर्शन किये थे। यहाँ परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर अपनी माता रेणुका का वध किया था तथा पिता जमदग्नि से प्राप्त वरदान से उनकी माँ पुनः जीवित हुई थी। इस स्थान से किलोमीटर दूर रेणुका का मंदिर भी है। परशुराम मंदिर में प्राचीन अष्ट धातु मूर्ति को लगभग ईसा से 576 वर्ष पूर्व के समय निर्मित्त मौर्यकालीन कला का प्रतीक माना जाता है।
दत्तात्रेय मंदिर
यह मंदिर मठ के आकार का है। इस मंदिर में आज से पच्चीस वर्ष पूर्व तक अष्ट धातु निर्मित भगवान बुद्ध की मूर्ति भी स्थापित थी, जिसे किसी ने चुरा लिया है। दत्तात्रेय महाभारत कालीन ऋषि थे और उन्होंने इसी स्थान पर तप किया था। बुद्ध भगवान की जो मूर्ति यहाँ से चोरी चली गयी है, उसे हर्ष के शासनकाल में हवेनसांग जब इस क्षेत्र में भ्रमण पर आया था तो उसने यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करवाई थी,क्योंकि दत्तात्रेय मंदिर का आकार एक मठ की तरह है और बौद्ध धर्म में भक्ति केन्द्र मठ ही होते हैं।
गोपेश्वर महादेव
भगवान शिव की आराधना का केन्द्र गोपेश्वर महादेव मंदिर माना गया है, इस क्षेत्र में जितने भी शिव मंदिर है उनमें सबसे बड़ा शिवलिंग इस मंदिर में स्थापित है। इस शिवलिंग में कुदरती त्रिशूल भी अंकित है। कहते हैं कि शिव ने जब अपनी आराधना में जगह-जगह विघ्नता महसूस की तो उन्होंने इस स्थान पर गोपी का रूप धारण कर तपस्या की जिससे इस स्थान का नाम गोपेश्वर महादेव पड़ गया।
जड़भड़त मंदिर
महाभारत के उपासना पर्व के अनुसार क्रीटस, उत्तकुरू, खस, त्रिसूज जातियाँ जब इस क्षेत्र में निवास करती थी तो उस काल में महासन्त जड़भड़त ने यहाँ तपस्या की थी और तपस्या करते-करते उन्होंने इस स्थान में ही समाधि कर ली थी। आज भी इनके समाधि स्थल पर प्राचीन मंदिर बना है।

मुखवा
यह स्थान भागीरथी नदी के दायें भाग पर विद्यमान है। इसकी प्राचीनता गंगोत्री धाम के समतुल्य है। यहाँ अधिकतर गंगोत्री मंदिर के पुजारी ही रहते हैं। जब गंगोत्री में अति हिमपात के कारण मंदिर के कपाट बन्द होते हैं तो उस समय मुखवा ग्राम में ही श्रीगंगा जी की चलमूर्ति की पूजा होती है।
पढ़ने के लिए क्लिक करेंः जानिए उत्तरकाशी जिले का इतिहास, पौराणिक महत्व और खासियत

लेखक का परिचय
लेखक देवकी नंदन पांडे जाने माने इतिहासकार हैं। वह देहरादून में टैगोर कालोनी में रहते हैं। उनकी इतिहास से संबंधित जानकारी की करीब 17 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। मूल रूप से कुमाऊं के निवासी पांडे लंबे समय से देहरादून में रह रहे हैं।
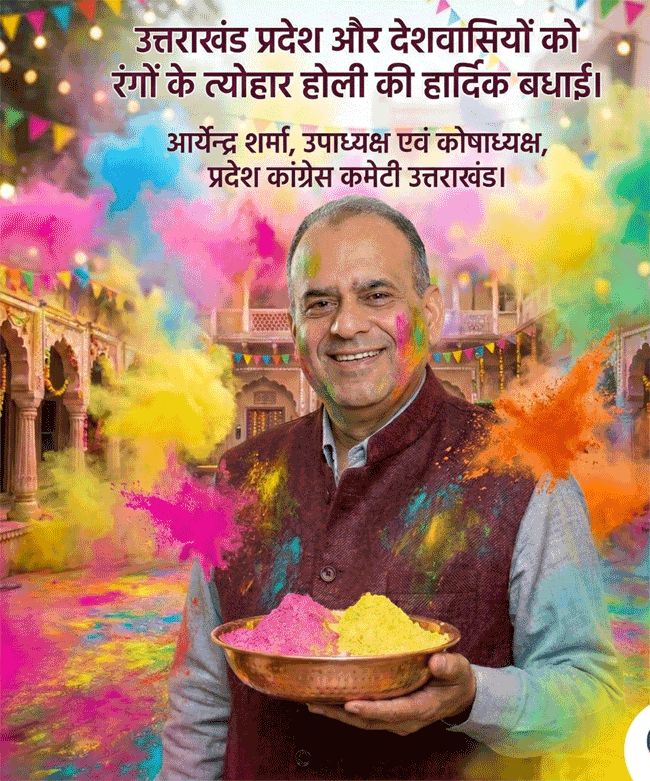
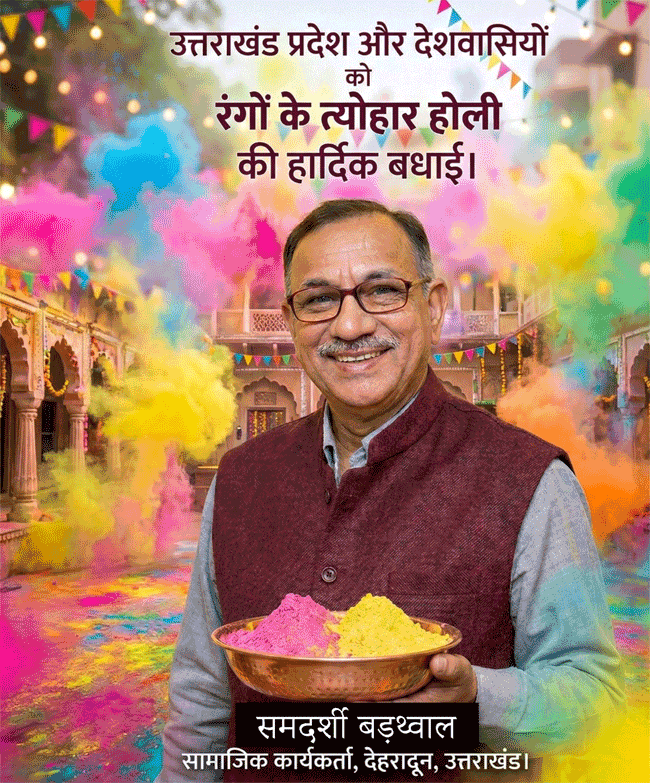
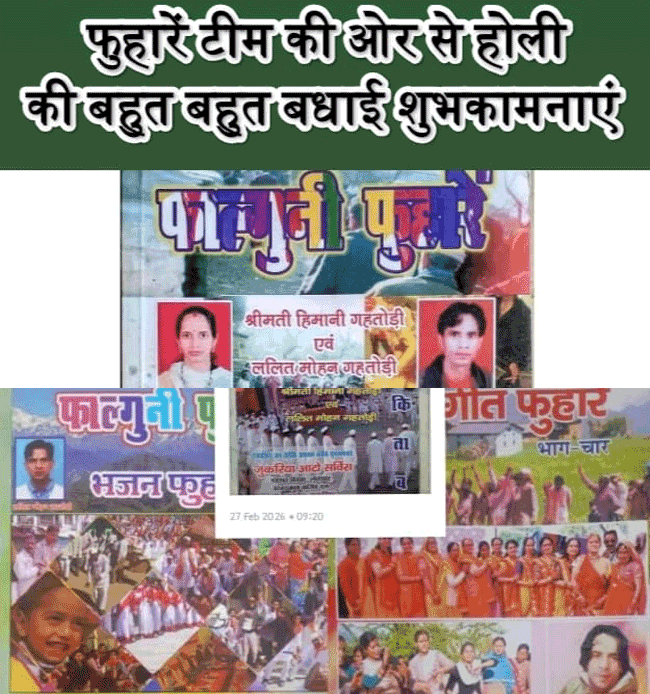
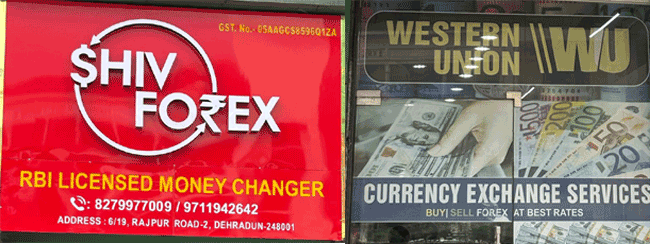








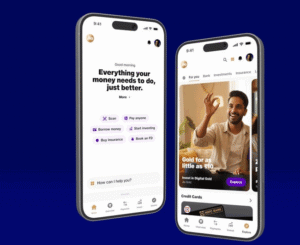
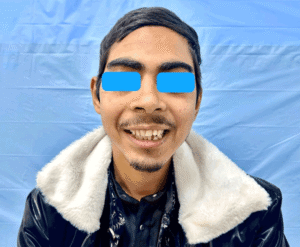

अति सुंदर जानकारी