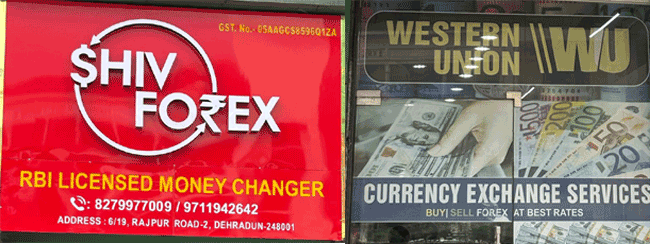बारह बजते ही तोप के धमाके से गरज उठती थी मसूरी, जानिए मसूरी का इतिहास, खासियत और रोचक जानकारी
लाखों पर्यटकों को आकर्षित करने वाली मसूरी सन्1826 तक वृक्षों व मंसूर झाड़ियों से ढकी हुई थी। आज पर्यटकों के लिए मसूरी एक शीतल, सुरम्य, सुहावना और आकर्षक नाम है। देहरादून के मस्तक पर ताज की तरह सुशोभित मसूरी की छटा अवर्णनीय है। जिस तरह देश के अन्य पर्यटक स्थल शिलांग, महाबलेश्वर, ऊटी तथा माउण्ट आबू में खुली, समतल भूमि देखने को मिल जाती है, वैसी मसूरी में नहीं है। यहां तो पहाड़ को काट-काट कर सड़क निर्मित की गयी है।
अंग्रेजों की पड़ी थी नजर
सन् 1814 या उसके आस-पास के वर्षों में अंग्रेजों की नजर मसूरी पहाड़ी पर पड़ी। अंग्रेज व्यवसायी, सैन्य अधिकारी, मिशनरी प्रचारक यहां आकर बसने लगे। यूरोपियन के लिये
अमोद प्रमोद का स्थान बनी मसूरी में अंग्रेजों ने अपनी खुशहाल शामों के लिये सर्वप्रथम हिमालयन क्लब की स्थापना की। सन् 1835 में मसूरी में एक स्कूल खोला गया, पर वह शीघ्र ही छात्रों के अभाव में बन्द हो गया, परन्तु भविष्य के लिए अनेक स्कूलों की परम्परा छोड़ता गया।
जहां कुमार दिलीप सिंह को रखा नजरबंद, अब है पांच सितारा होटल
1836 में बंगाल इंजीनियर्स सैन्य दल के कैप्टन रैनी टेलर ने क्राइस्ट चर्च नामक प्रथम गिरजाघर बनवाया। 1853 में ब्रिटिश शासकों ने मसूरी के कैसल हिल नामक बंगले में पंजाब के गौरव राणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कुमार दिलीप सिंह को नजरबंद करके कई वर्ष तक रखा था। यह कैसल हिल बार्लोगंज में बहुत समय तक एक खण्डहर के रूप में रहा, परन्तु अब जेपी रेजीडेन्सी मैनर के नाम से पांच सितारा होटल में परिवर्तित हो गया है।
मसूरी का पहला होटल बना लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी
मसूरी में सबसे पहले चालविले नामक होटल अंग्रेज व्यवसायी हॉबसन के दो पुत्र चार्ली और विली के नाम पर खोला गया। यही चालविले होटल आज लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी के रूप में प्रशासकीय सेवाओं के लिए युवक युवतियों को प्रशिक्षित करने का संस्थान है।

सुविख्यात लेखक राहुल सांकृत्यायन का आवास
हैप्पी वैली, बहुत लम्बे समय तक सुविख्यात लेखक राहुल सांकृत्यायन के आवास के रूप में पहचानी जाती रही। राहुल सांकृत्यायन की कथाओं में मसूरी का 1950 के आसपास का वर्णन पढ़कर, अतीत जो मसूरी खो चुकी है, बरबस ही स्मृति पटल में चित्रांकित होने लगता है। राहुल जी के शब्दों में- 1945 के दिसम्बर की तारीख है, आज जितनी बर्फ पड़ी है शायद इस वर्ष की सबसे बड़ी हिमवृष्टि है। हैप्पी वैली मोहल्ले में आने जाने वाले बहुत कम ही है। इसीलिए लोगों के पैरों ने बर्फ को दबा कर रास्ता पकड़ा। वहां अछूती बर्फ पर डेढ़ दो सौ गज चलना पड़ा। सड़क तक पहुंचने में हमें कष्ट और थकावट मालूम पड़ी। सड़क से आज पच्चीस-पचास आदमी जरूर गुजरे थे। इसीलिए उनके पैरों ने बर्फ को दबाकर एक फुट चौड़ा रास्ता बना दिया था। आमने सामने से आने पर किसी को बगल में हाथ भर बर्फ में धंसकर रास्ता छोड़ना पड़ता। ऐसी थी पर्वत रानी मसूरी।
स्टोक्स स्कूल बना सेवाय होटल
अंग्रेज मैडोक्स ने स्टोक्स स्कूल खोलकर भले ही मसूरी को स्कूलों का शहर बना दिया, परन्तु अपने इस प्रचलित स्कूल को लखनऊ के एक रईसजादे को बेचकर उसे होटल का रूप दिलाने में मैडोक्स चाहे प्रशंसा के पात्र न बने हों पर देश-विदेश के पर्यटकों के लिए एक ऐसी आवासीय सुविधा छोड़ गए हैं जो आज ‘सेवाय’ होटल के नाम से व्यवसायिक प्रसिद्धि पाए हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों तक सैवाय होटल कैबरे डान्स के कारण आकर्षण
का केन्द्र बना रहा।
बारह बजने की जानकारी दी जाती थी तोप के धमाके से
बारह बजने का ज्ञान मसूरी वासियों को बहुत लम्बे समय तक तोप के धमाके से कराया जाता था। यह तोप, गन-हिल से दागी जाती थी। मसूरीवासियों द्वारा तोप की आवाज के विरोध में लगातार नारेबाजी का स्वर प्रकट करने पर 1919 में तोप दागने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी तथा उसके स्थान पर रात्रि नौ बजे प्रकाश व्यवस्था को मद्धिम कर समय का भान कराया जाने लगा।

गन हिल तक रोपवे है आकर्षण
गन हिल में आज मसूरीवासियों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का कृत्रिम जलाशय है। यहां तक पहुंचने के लिए दो किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, परन्तु 1970 में मसूरी नगरपालिका ने यहां तक पहुंचने के लिए ‘रोपवे’ की व्यवस्था कर दी। गन हिल से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
पहाड़ों की रानी
अपनी प्राकृतिक सुषमा के कारण ही मसूरी हिल स्टेशनों की रानी कहलाती है। यहां की माल रोड पर सायंकाल बड़ी भीड़ रहती है। इसी भीड़ को लेकर बड़े-बूढ़े आज भी कह उठते हैं कि जब तक कंधे से कंधा न टकराए तो मसूरी आने का लाभ क्या?

मसूरी के लिए पैदलयात्रा
सन् 1930 से पूर्व जब मसूरी के लिये मोटर मार्ग न था, पर्यटक या स्थानीय लोग मसूरी, पैदल मार्ग से ही पहुँचा करते थे। देहरादून से राजपुर तक जाने के लिये मोटर कार व तांगा ही यातायात का साधन था। पूरे तांगे का किराया बारह आना तथा पूरी कार का 6 रूपया था। राजपुर से पैदल मार्ग के लिये चढ़ाई आरम्भ होते ही पथकर चुंगी कार्यालय के समक्ष से गुजरना पड़ता था। वहीं नियत शुल्क का भुगतान कर आगे बढ़ा जा सकता था। पैदल मार्ग से मसूरी पहुंचने वाले की चुंगी भुगतान पर्ची की जांच परख का काम झाडीपानी में होता था। झड़ीपानी में एक आराम गृह व इस्टर्न इण्डिया रेलवेद्वारा संचालित स्कूल था। जो बाद में ओक ग्रोव स्कूल कहलाया।

झड़ीपानी जहां था नेपाला राजपरिवार का पैलेस
झड़ीपानी से दो फलांग मसूरी की और नेपाल राजपरिवार का फेयरलान पैलेस था जो उस समय सम्पूर्ण मसूरी में विशालतम भवन था। फेयरलान से डेड किलोमीटर तक समतल सड़क तथा उसके बाद बालोगंज। वालोगंज पहुंचने पर एक छोटा बाजार, जिसमें दो जलपानगृह, डाकतार घर, गुरुद्वारा, सेन्ट फिडलिस हाइस्कूल तथा सैंट जॉर्जेज कॉलेज थे। यहां पर एक प्रसिद्ध झूला पुल भी आकर्षण केन्द्र था, जो आज भी मात्र दर्शनार्थ उपलब्ध है। यहां से मसूरी के लिए तीन किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई है, लेकिन यात्री इस चढ़ाई से हतोत्साहित नहीं होता, क्योंकि उसे मसूरी पहुंचने का आभास उत्साहित किए रहता है।
मोटर कार से मसूरी पहुंचने का मार्ग
राजपुर से मसूरी की ओर मोटर बस या कार से जाने वाले यात्री प्राय: सड़क को देखते ही पूछ लिया करते थे, यह सड़क कब तथा किसने बनाई। इस सड़क को बनाने का श्रेय इंजीनियर जॉन मेकिनॉन को जाता है। जॉन मेकिनॉन ने पैदल निरीक्षण कर राजपुर से कोल्हू खेत तक के सड़क निर्माण को कई बार कागजों में उकेरा तथा उसके बाद इसको कार्य रूप में परिवर्तित किया। बरसात में भूस्खलन के कारण यह मेकिनॉन कार्ट रोड कई बार बीच में ही रोक देनी पड़ी।

व्हैंपर एण्ड कम्पनी ने इस सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये सन् 1876 में जॉन मेकिनॉन से लइसे लीज में लिया, तथा मरम्मत कर ब्रुकलैण्ड्स एस्टेट तक निर्मित किया। इस तरह जॉन मेकिनॉन और व्हैंपर एण्ड कम्पनी के सहयोग से यह दुर्गम कार्य सम्पन्न हो सका।
लम्बे समय तक वह सड़क कार्ट रोड के रूप में ही उपयोग में लाई जाती रही। लेकिन सन् 1926 में संयुक्त प्रांत स्वायत शासन मंत्री सर मोहम्मद युसूफ ने सरकारी सहायता से इस मेकिनॉन कोर्ट रोड को मोटर कार सड़क के रूप में निर्मित कराने में सहयोग किया। कुछ समय उपरान्त कोल्हू खेत तक पहुंचने वाले मोटर मार्ग को भट्टा गांव तक पहुंचाया गया।
एक रुपया सीट था मोटर का किराया
उस समय मोटर द्वारा देहरादून स्टेशन से भट्टा गांव तक पहुंचने के लिये यात्रियों को एक रूपया प्रति सीट किराया देना पड़ता था। भट्टा से मसूरी तक जाने के लिये यात्री को या तो पैदल राह पकड़नी पड़ती थी या फिर 5 या 10 रूपया हाथ रिक्शा को देकर मसूरी पहुंचा जा सकता था। सन् 1929-30 में भट्टा से मसूरी तक सड़क निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ। अब देहरादून से मोटर द्वारा मसूरी तक पहुंचने के लिये डेढ घंटे का समय लगने लगा। मोटर बस, जिसमें दो प्रकार को बैठने की व्यवस्था थी। लोवर एण्ड अपर। टिकट दर भी उसी प्रकार निश्चित थी। एक रूपया बारह आने लोवर क्लास तथा तीन रुपया अपर क्लास सीट। अगर यात्री, कार का किराया वहन करने में सक्षम होता तो उसे पूरी टैक्सी का किराया देहरादून से मसूरी तक का 25 रूपया अदा करना होता था।

पथकर व्यवस्था
कोल्हू खेत में मसूरी नगरपालिका द्वारा यात्रियों से पथकर लिये जाने की व्यवस्था थी। यहां 1 रूपया 8 आने प्रति बस यात्री तथा 2 रूपया प्रति टैक्सी कार यात्री पथकर लिया जाता था। पथकर भुगतान से केवल मसूरी नगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी व देहरादून के सरकारी अधिकारी ही छूट प्राप्ति के हकदार थे। गर्मियों में यातायात की सघनता को देखते हुए उसे व्यवस्थित करने के उद्देश्य से ‘गेट’ पद्धति लागू की गयी। राजपुर से गेट नियंत्रित होता था। इस तरह वन-वे ट्रैफिक को व्यवस्था कई वर्षों तक लागू रही। बाद में इसे राजपुर से हटा कर कोल्हू खेत तथा कुछ वर्षों के उपरान्त किंक्रेग में स्थानान्तरित कर दिया गया था। किंक्रेग से पिक्चर पैलेस जाने वाले मार्ग का नियंत्रण 1983 तक गेट पद्धति से ही संचालित होता रहा।
इन विभूतियों ने मसूरी के विकास में की सेवा
सन् 1942 के आसपास मसूरी में कुछ ऐसी विभूतियाँ थीं जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक मसूरी के विकास के लिए निस्वार्थ भावना से सेवा की। उनमें प्रमुख इस प्रकार थे- सर्व श्री पुष्कर नाथ तन्ना, कैप्टन कृपाराम, गोपालदत्त डिमरी, डॉ. कुशलानन्द गैरोला, जगन्नाथ पाँधी, रामकृष्ण वर्मा तथा पी.सो.हरि।
कुलियों ने किया था मोटर मार्ग का विरोध
सन् 1954-55 में किंक्रेग से मॅसानिक लॉज मोटर मार्ग निर्माण के समय वहाँ के कुलियों, डाँडी, कण्डी व रिक्शा चालकों ने विरोध किया परन्तु रामकृष्ण वर्मा मोटर मार्ग निर्माण के लिए कटिबद्ध थे। परिणामत: मोटर मार्ग निर्माण ने विरोध के बावजूद भी स्वरूप लिया। गोपालदत्त डिमरी मजदूरों के परम हितैषी थे। उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों तक यहाँ के मजदूर वर्ग को जहाँ अनुशासित रखा वहीं कभी उनका शोषण भी नहीं होने दिया। उनकी मृत्यु के बाद पातीराम डोभाल ने मजदूर संघ के विकास की भूमिका का डिमरी के अनुरूप अंतिम क्षणों तक निर्वहन किया।
इनका भी रहा योगदान
गाँधी चौक क्षेत्र के विकास के लिए पुष्करनाथ तन्खा व कैप्टन कपाराम की सेवायें आज भी स्मरण की जाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में श्री राधा बल्लभ खण्डूरी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अपने स्वर्गीय भ्राता घनानन्द खण्डूरी की स्मृति में मसूरी के गरीब विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की स्थापना लण्डौर स्थित कोहिनूर बिल्डिंग में की थी, जो सन् 1944 मे किंक्रेग के समीप एक पुराने भवन में स्थानान्तरित किया गया। सरदार बलवंत सिंह स्याल, हामिद हसन, सत्यप्रसाद थपलियाल जैसे अनुशासन प्रिय प्रधानाचार्य इस विद्यालय में रहे हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दौर में जब मसूरी अपने शैशव काल में थी, उस समय क्षेत्र में जल के प्राकृतिक 88 स्त्रोत थे। आज उचित देखरेख के अभाव में घटकर मात्र 17 रह गये हैं।
मसूरी में शराब कारखाना
आज से 190 वर्ष पूर्व मसूरी में भारत का सबसे पहला शराब का कारखाना खोला गया था। अंग्रेज अपने सैन्य अधिकारियों को प्रतिदिन शराब परोसते थे। बाहरी मुल्कों से मंगाई गयी शराब काफी महंगी पड़ती थी। इसलिए मेरठ के एक अंग्रेज साहूकार हेनरी बोहले ने सन् 1830 में हाथी पाँव क्षेत्र में ओल्ड ब्रुअरी के नाम से बीयर का कारखाना स्थापित किया था। कारखाना चलने के कुछ समय पश्चात् हेनरी बोहले ने सैन्य अधिकारियों को माँग पर शराब की आपूर्ति भी शुरू कर दी। एक वर्ष बाद सन् 1831 में लंढौर छावनी प्रमुख कैप्टन यंग ने हेनरी बोहले पर जाली परमिट का आरोप लगाते हुए 24 अप्रैल 1831 को कारखाना बन्द करा दिया। बाद में यही कारखाना पार्सन ने खरीदा, लेकिन 1834 में पार्सन ने इसे जॉन मैकिनॉन को बेच दिया। जॉन मैकिनॉन ने बार्लोगंज क्षेत्र में सन् 1842 में पानी के एक प्राकृतिक स्त्रोत के समीप क्राउन ब्रुअरी के नाम से बीयर फैक्ट्री खोली। बाद में इस कारखाने में हिवस्की वरम का भी उत्पादन किया जाने लगा। क्राउन ब्रुअरी में निर्मित शराब इतनी लोकप्रिय हो चुकी थी कि इसके वितरण के लिए बंबई, मद्रास दिल्ली व जबलपुर के व्यसायी लाइन लगाए बैठते थे।
हिक्स थर्मामीटर
बार्लोगंज क्षेत्र में सन् 1862 में हिक्स थर्मोमीटर्स इंडिया लिमिटेड स्थापित किया गया था। हिक्स ने सन् 1895 में अपने नाम से थर्मोमीटर का पेटेंट कराया। हिक्स की गिनती आज भी विश्वसनीय थर्मोमीटर निर्मित करने वालों में की जाती है।
मसूरी नगरपालिका
उत्तर प्रदेश की प्रथम और देश की दूसरी नगरपालिका मसूरी का जन्म 160 वर्ष पूर्व सन् 1850 में हुआ था। इसके पहले चेयरमैन मेजर फ्रुथ नियुक्त हुए थे। उस समय विभिन्न कार्यक्षेत्रों के दक्ष व्यक्ति नगर पालिका सदस्य हुआ करते थे। 1850 में ही मसूरी पालिका को ‘ए’ श्रेणी की पालिका होने का गौरव प्राप्त हो गया था। स्थापना वर्ष से ही शिक्षा, जल, विद्युत्त आदि व्यवस्थायें पालिका के पास थी। इस व्यवस्थाओं के रहते पालिका को कमी धनाभाव नहीं रहा।
आजादी से पूर्व व बाद के वर्षों तक नगरपालिका के नियम सख्ती के साथ लागू किये जाते थे। स्वच्छ और शोरगुल रहित मसूरी में साधारण आदमी तो क्या विशिष्ट व्यक्ति को भी नियमों के विपरीत कार्य करने का साहस नहीं होता था।

पालिका की सख्ती के आगे नेहरू भी हुए मजबूर
नगरपालिका के सख्त नियमों का ही परिणाम था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नहेरू को भी मालरोड पर पैदल ही चलना पड़ा था। आजादी के दो दशक बाद तक भी पालिका एक सम्पन्न इकाई के रूप में पर्यटक व मसूरी वासियों की भरपूर सेवा करती रही। बाद के वर्षों में पालिका के अधिकारों में कटौती की जाने लगी। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था 1968 में पालिका से लेकर बेसिक शिक्षा परिषद के सुपुर्द कर दी गयी। विद्युत्त व्यवस्था सन् 1976 में उत्तर-प्रदेश विद्युत्त परिषद को सौंप दी गयी। 1975 में जलापूर्ति भी गढ़वाल जलसंस्थान को हस्तान्तरित कर दी गयी। आय स्त्रोत की इन तमाम व्यवस्थाओं को दूसरे विभागों को हस्तान्तरित करने के बाद नगरपालिका की आर्थिक हालत बिगड़ती चली गयी। परिणामत: नागरिक व पर्यटकों को मूल सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए पालिका को राज्य सरकार पर आश्रित रहने को बाध्य होना पड़ा। मसूरी पालिका की वह गौरव गरिमा जो ब्रिटिश काल में थी आज धूल-धुसरित हो चुकी है।
पालिका के प्रशासक व अध्यक्ष
स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद वर्ष 1947 में श्री रफी अहमद किदवई मसूरी पालिका के पहले भारतीय प्रशासक नियुक्त हुए। सन् 1957 में रामकृष्ण वर्मा इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने। उसके बाद जगन्नाथ शर्मा (1957-64), सुश्री सत्या सूद (1965-66), हुक्म सिंह पंवार (1967-71), भोला सिंह रावत (1971-75), जोधसिंह गुनसोला सन् 1988 व 1997 में दो बार पालिकाध्यक्ष निर्वाचित हुए।
बदहाल होती गई पालिका
60.08 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की व्यवस्थायें संभाल रही मसूरी पालिका के लिए पुराने गौरवशाली दिन अब मात्र इतिहास के पृष्ठों में सिमट कर रह गये हैं। मसूरी पालिका की बदहाली के लिए मुख्य रूप से लोटिंग पापुलेशन जिम्मेवार है। पालिका को इस लोटिंग पापुलेशन से आर्थिक लाभ मिलना तो दूर इसके विपरीत उन्हें मूलभूत समस्त सुविधायें उपलब्ध करानी पड़ती हैं।

मसूरी के चर्च
अंग्रेजों ने लाइब्रेरी बाजार के समीप क्राइस्ट चर्च का निर्माण किया। वस्तुत: यह मसूरी का पहला चर्च था, जिसे स्थानीय जनता आम भाषा में लाट चर्च भी कहा करती थी। इस चर्च को 1838 में बंगाल इन्जीनियर ग्रुप के कैप्टन रेसी टेलर ने चर्च आफ इंग्लैण्ड के अधीन बनाया। इसके बाद तो अकेले मसूरी में 19 चर्च बनाये गये, जिनमें सात चर्च तो ध्वस्त हो चुके हैं।
मसूरी में एक चर्च ऐसा भी है जो भारतीय परम्पराओं और आस्थाओं को समेटता हुआ भारतीयों के सहयोग से चलता है। यह चर्च है ‘ मेमोरियल मैथेडिस्ट चर्च’ जिसकी स्थापना डेनिस ऑसवन ने 28 मई सन् 1885 में की थी।

यह चर्च किसी विदेशी सहायता पर नहीं अपितु चर्च से जुड़े सदस्यों के सहयोग से चलता है। चर्च के अध्यक्ष स्वयं पादरी हैं तथा संचालन के लिए एक समिति है। चर्च की समिति धार्मिक कार्यों के साथ-साथ सामाजिक कार्यों को भी प्रोत्साहित करती है। चर्च की अनोखी परम्परा यह है कि जब कोई मसूरी का विशिष्ट व्यक्ति स्वर्ग सिधारता है तो चर्च की ओर से
उसको आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना आयोजित की जाती है। यहाँ सभी प्रार्थनायें हिन्दी में होती हैं। इसाई समुदाय के विद्यार्थियों को शैक्षिक प्रोत्साहन हेतु चर्च द्वारा छात्रवृत्ति भी दी जाती है।
तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी
मसूरी का किताबघर जो गाँधी चौक भी कहलाता है, कभी यहाँ एक समतल मैदान था। जहाँ देहरादून के तत्कालीन सुपरिन्टेन्डेन्ट बैंसीटार्ट ने 18 अप्रैल 1843 को स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना की थी। इस लाइब्रेरी के एक मंजिले भवन के निर्माण में उस समय डेढ़ वर्ष का समय लगा था। उन दिनों मसूरी स्टेशन कहलाता था अत: इसे स्टेशन लाइब्रेरी तथा बाद में मसूरी लाइब्रेरी का नाम दिया गया। अंग्रेजी शासकों की संकीर्ण मानसिकता की द्योतक मसूरी लाइब्रेरी लम्बे समय तक योरोपियन समुदाय के लिए ही खुलती रही। इस लाइब्रेरी के आरम्भ होने के 43 वर्षों बाद सन् 1886 में बहुत विचार विमर्श के पश्चात् एंग्लो इण्डियन समुदाय को प्रवेश की अनुमति मिल सकी। 1843 से लेकर 1920 तक किसी भारतीय को इस लाइब्रेरी से प्रवेश की अनुमति देना तो दूर की बात, सूचना पट्ट लगाकर उसे अपमानित भी किया जाता रहा।

मनमानी के विरोध में बनी तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी
मसूरी लाइब्रेरी के संचालक मंडल की मनमानी के विरूद्ध तथा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मसूरी के गणमाण्य भारतीयों ने इसके समकक्ष एक ऐसी लाइब्रेरी बनाने पर विचार किया जिसमें समस्त भारतीय सम्मान के साथ प्रवेश कर सकें। 15 अगस्त सन् 1920 को लोकमान्य तिलक को श्रद्धांजलि देने हेतु मंशाराम बैंक के स्वामी लाला महावीर प्रसाद के निवास पर बैठक के दौरान लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया तथा तिलक मेमोरियल कमेटी का गठन किया गया। इस बैठक में पंडित आनन्द नारायण के अतिरिक्त एच.बी.एस. डालीवाल, नारायण लाल, डॉ0 एम.ए.शाह, पंडित ज्ञान चंद्र, लाला महावीर प्रसाद, ब्रिजनाथ, इलाही बख्श, बाबू गोपाल सिंह, एस.एन.मेहरा आदि ने भाग लिया। इस पहली बैठक में ही लाइब्रेरी प्रारम्भ करने हेतु 1972 रूपये का चन्दा भी एकत्रित हुआ। पंडित घनानंद के सहयोग से 23 अक्टूबर सन् 1920 को मैटसन लॉज, जोकि एक होटल था खरीदा गया और तिलक की स्मृति में ‘तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी’ का उद्घाटन हुआ।
बदलता रहा लाइब्रेरी का भवन
कुछ वर्षों के उपरान्त 8 सितम्बर 1923 को मैटसन लॉज को अपरिहार्य कारणों से बेच देना पड़ा। अतः लाइब्रेरी को लंदन हाउस में स्थानान्तरित कर दिया गया। तदुपरान्त कुछ वर्षों तक पल्विना हाउस रिंक के पास लाइब्रेरी अस्थायी रूप से संचालित की जाती रही। लाइब्रेरी कमेटी ने स्थायी हल ढूंढने के उद्देश्य से सिल्वरटन एस्टेट की कुछ भूमि खरीदकर उस पर हालनुमा भवन निर्मित कराया। 4 अप्रैल सन् 1941 को लाइब्रेरी को स्थायी रूप से वहाँ स्थापित कर दिया गया। श्रीपुष्करनाथ तन्खा इसके सचिव नियुक्त हुए और चालीस वर्षों तक निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे। आज तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी के साठ आजीवन सदस्य तथा दो सौ के लगभग साधारण सदस्य है, वर्तमान में लाइब्रेरी में लगभग पचास हजार पुस्तकों का संग्रह है।

लेखक का परिचय
लेखक देवकी नंदन पांडे जाने माने इतिहासकार हैं। वह देहरादून में टैगोर कालोनी में रहते हैं। उनकी इतिहास से संबंधित जानकारी की करीब 17 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। मूल रूप से कुमाऊं के निवासी पांडे लंबे समय से देहरादून में रह रहे हैं।