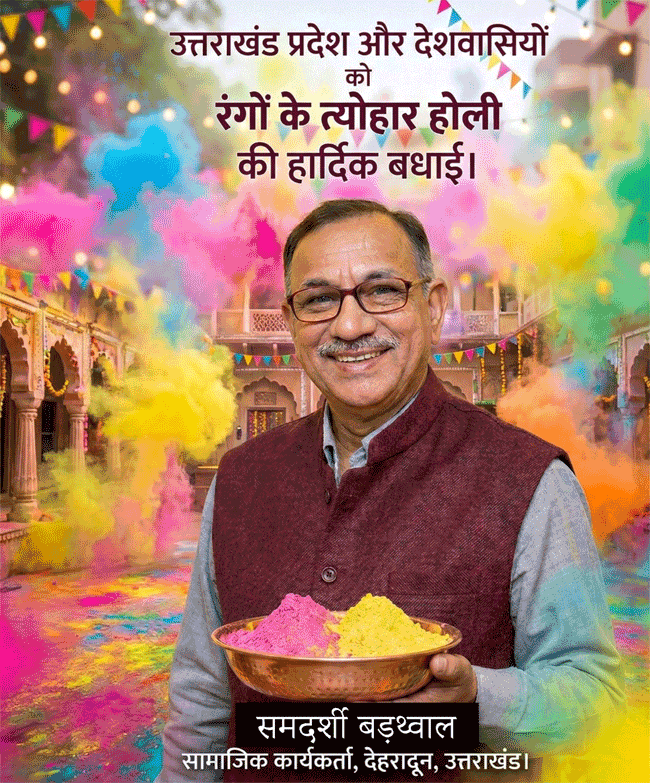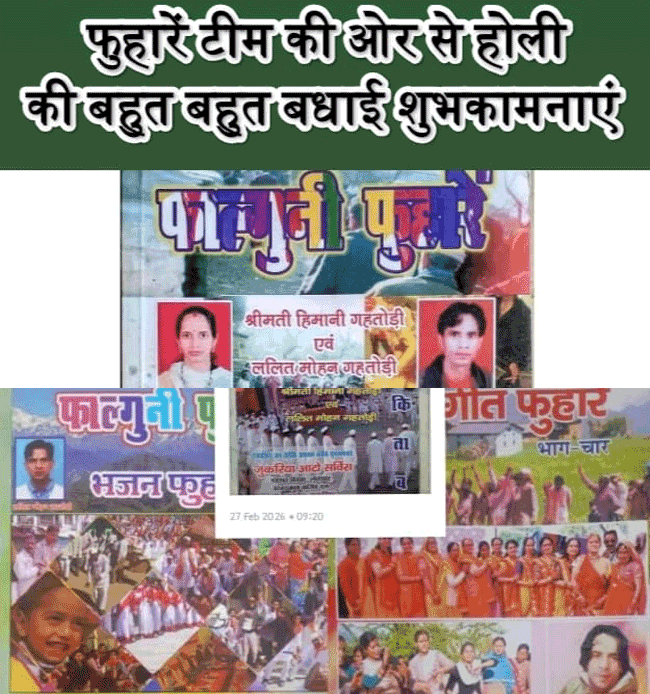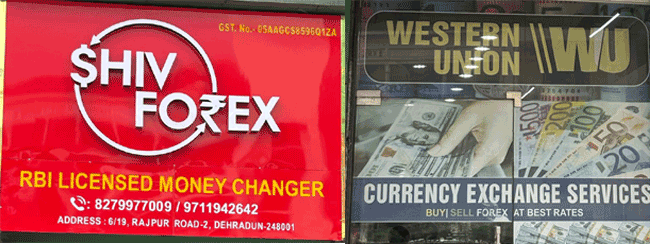यहां केदारनाथ मंदिर से भी है प्राचीन मंदिर, विद्यमान हैं दुर्लभ प्रतिमाएं
उत्तराखंड में हर जिले में प्राचीन मंदिरों के साथ ही पर्यटन स्थल काफी संख्या में मिल जाएंगे। ऐसे कई स्थलों तक पहुंचने के लिए रोमांच का सफर तय करना पड़ता है। कठिन दुर्गम रास्तों का सफर तय करने के बाद ही मनोरम दृश्यों का अवलोकन होता है। जहां लगता है कि इससे सुंदर संसार में और कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग जनपद की। यहां चारधामों में से विश्वप्रसिद्ध केदारनाथ धाम है। इस धाम के अलावा भी जनपद में कई ऐसे मंदिर हैं, जो कि काफी प्राचीन हैं। आइए हम आपको रुद्रप्रयाग जनपद के मंदिरों और पर्यटन स्थलों के बारे में बताते हैं।
केदारनाथ से भी प्राचीन मंदिर
रुद्रप्रयाग जनपद में ऊखीमठ से आठ किलोमीटर आगे मनसूना गाँव स्थित है। मद्महेश्वर मंदिर की यात्रा का पहला रात्रि पड़ाव मनसूना गाँव है। गाँव से सुबह की ठंडी हवा की यात्रा और चौखम्भा शिखर के पीछे से आती प्रात:काल की धूप उसके श्रृंगों को आलोकित करती हुई दृष्टिगत होती है। यात्रा के दौर में पहला गाँव पाँच किलोमीटर की दूरी पर जुगासू, तदुपरान्त मद्महेश्वर गंगा को पार कर सीधी चढ़ाई के मार्ग में उन्याणा गाँव और फिर रासी गाँव पड़ता है। रासी गाँव में राकेश्वरी देवी का अत्यन्त प्राचीन व विशाल मन्दिर स्थित है, जिसमें अनेक दुर्लभ प्रस्तर प्रतिमायें विद्यमान हैं। कहते हैं कि यह मन्दिर, केदारनाथ मन्दिर से भी प्राचीन है। यहीं पर चन्द्रदेव ने राकेश्वरी माता की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था।

सैकड़ों वर्ष से सुलग रही धूनी
मन्दिर के अन्दर एक अखण्ड धूनी आज भी सैकड़ों वर्ष से सुलग रही है। प्रतिवर्ष पूरे श्रावण माह में स्थानीय ग्रामवासी यहाँ श्रद्धापूर्वक देवी की पूजा-अर्चना करने पहुँचते हैं। रांसी से आगे की ढलानपूर्ण नौ किलोमीटर यात्रा के पश्चात् मद्महेश्वर गंगा व मरणी नदी के संगम पर स्थित अंतिम गाँव गौंडार दिखता है। गौंडार से आगे एक घंटे की खड़ी चढ़ाई के बाद खंडाराखाल आता है। खंडाराखाल में दुकान है, जहाँ खाने से लेकर रात्रि विश्राम तक को सुविधा उपलब्ध है। खंडारा से बौज बुरांश के घने जंगलों के बीच से सीधी चढ़ाई वाला दस किलोमीटर का मार्ग तय कर मद्महेश्वर मन्दिर के शिखर के दर्शन होते हैं।
मद्महेश्वर मंदिर
कैलाश पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में 10853 फीट की ऊँचाई में यह मन्दिर अवस्थित है। मन्दिर में भगवान शिव, लिंग के रूप में विराजमान हैं। मन्दिर एवं मन्दिर परिसर में क्षेत्रपाल भैरव आदि के पूजा स्थल है। मन्दिर मई माह से नवम्बर तृतीय सप्ताह तक खुला रहता है। कपाट बन्द होने पर मध्यमहेश्वर की डोली ऊखीमठ आ जाती है। शीतकाल में इसकी पूजा औंकारेश्वर मन्दिर ऊखीमठ में की जाती है। मद्महेश्वर मन्दिर के चारों ओर प्राकृतिक सम्पदाओं का भंडार है। मध्यमहेश्वर के लिए एक मार्ग ऊखीमठ से मनसूना-राँसी-गौंडार होते हुए जाता है। दूसरा मार्ग केदारनाथ मार्ग के रास्ते में पड़ने वाले गुप्तकाशी से भी जाता है।

सघन जंगल के बाद वृक्ष सीमा समाप्त होते ही एक छोटे से बुग्याल में पंचकेदार में एक मध्यमहेश्वर का प्राचीन व विशाल मन्दिर दर्शनीय है। मुख्य मन्दिर के प्रांगण में ही स्थित दो छोटे-छोटे मन्दिरों में शिव-पार्वती की अत्यन्त कलात्मक मूर्तियाँ रखी हुई हैं। मुख्य मन्दिर के अन्दर स्थित शिवलिंग एक ओर को झुका व फटा हुआ है। दंत कथाओं के अनुसार तिब्बत के एक राजा की गाय यहाँ आकर लिंग के ऊपर दूध चढ़ाया करती थी। गाय के इस कृत्य से क्रोधित राजा ने दूध चढ़ाते समय गाय पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया। गाय द्वारा तत्काल स्थान छोड़ जाने से कुल्हाड़ी का प्रहार सीधा शिवलिंग पर हुआ, जिससे उसका तिरछा व कटा हुआ स्वरूप बन गया। गाय के खुरों के चिह्न आज भी मन्दिर प्रांगण में विद्यमान हैं।
बुग्यालों का मनोरम दृश्य
रात्रि विश्राम मद्महेश्वर में कर प्रात:काल प्रस्थान करने पर ही पाँच घंटे की लगातार कठिन यात्रा के उपरान्त दोपहर एक काछनीखाल (13200 फीट) पहुँचा जा सकता है। इस स्थान से नीचे की ओर देखने पर मध्यमहेश्वर सघन वन तथा दूसरी ओर मौर्लो लम्बे बुग्यालों का दृश्य बड़ा ही मनोरम लगता है। मार्ग में भेड़-बकरियों के रुकने के चिह्न दिखते रहते हैं। इनसे ही ज्ञान होता है कि यात्री गन्तव्य स्थान के लिए सही मार्ग पर चल रहा है। ऐसे स्थल जो भेड़-बकरियों के रुकने के चिह्न देते हैं, स्थानीय भाषा में खर्क कहलाते हैं।

यहां है रंगबिरेंगे फूलों का सागर है पांडवसेरा बुग्याल
मार्ग में आने वाले हर पहाड़ी नाले को पार करने के लिए प्रत्येक बार नीचे की ओर आना पड़ता है और नाले के दूसरी ओर फिर होता है सामना विकट चढ़ाई से। ऐसे कई उतार-चढ़ाव में यात्री थकान का अनुभव निर्धारित विश्राम-स्थल से पूर्व ही करने लगता है। एक-दो स्थानों पर तो उफनते कमर तक गहरे पानी को फिसलन भरे पत्थरों में पैर जमाते हुए पार कराना पड़ता है। सूर्य ढलने से पहले ही पाण्डवसेरा का विशाल बुग्याल दिखने लगता है। यह बुग्याल चारों ओर असंख्य रंग-बिरंगे फूलों का एक सागर सा दिख पड़ता है। यहाँ भेड़-बकरी चराने वाले पालसियों के लगे शिविर ही एकमात्र विश्राम स्थल हैं।
पहाड़ी गुफा में ही शिविर लगाकर रात्रि विश्राम किया जा सकता है। पाण्डसवेरा के विशाल बुग्याल का अवलोकन किये बिना प्रकृति की अनुपम सौगात से मुंह मोड़ना होगा। अब यहाँ पालसी ही वनस्पति व दृश्यों के बारे में उचित जानकारी दे सकता है। अत: मीलों तक फैले पाण्डवसेरा बुग्याल को घूमने के लिए पालसियों का मार्गदर्शन आवश्यक है। बुग्याल के दूसरे सिरे पर ग्लेशियर से निकलने वाली मध्यमहेश्वर गंगा का दृश्य बड़ा अचरजपूर्ण है।
यहाँ मध्यमहेश्वर गंगा ने सीधी खड़ी चट्टान को गहराई तक काटकर उसमें गहरी और तंग आड़ी-तिरछी बाटी बना रखी है। पालसी के अनुसार नदी में बहकर आने वाले रत्नों ने यह चट्टान इतनी गहराई तक काटी है। विकट यात्रा की सुखद एवं अविस्मरणीय दूसरी रात्रि भी पाण्डवसेरा की पहाड़ी में व्यतीत कर प्रात:काल नन्दीकुंड के लिए प्रस्थान करना समयोचित विचार है। मार्ग में उफनती मध्यमहेश्वर गंगा को मात्र दो विशाल पत्थरों के ऊपर से पार करना खतरे से खाली नहीं लगता।
यहां पांडवों ने बनाए थे धान के खेत
अभी बुग्याल की सीमा समाप्त नहीं हुई कि धान के खेत की तरह कुछ खेत दिखायी पड़ने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अज्ञातवास के समय पाण्डवों ने ही धान के यह खेत बनाये थे। इन खेतों के समीप ही चट्टान के नीचे से निकलती जल की धारा, छोटी-छोटी नहरों में परिवर्तित हो प्रवाहित होती दिखती है। जो आश्चर्यजनक लगता है। शायद पाण्डवों ने धान के खेतों को सींचने के लिए यह व्यवस्था बनाई हो। पहाडी घाटी से आती जलधारा के किनारे किनारे लगभग चार किलोमीटर चलने पर नन्दीकुंड के दर्शन होते हैं।

साहसी यात्री को मिलता है नंदी कुंड देखने का सौभाग्य
मार्ग में विशालकाय शिलाओं को पार करते हुए हल्के नीले रंग के पानी का विशाल लम्बा विस्तार दिखाई देता है, वही है नन्दीकुंड। चारों ओर मनमोहक दृश्य, बायीं ओर के तट पर प्राइमुला के पुष्प का लम्बा विस्तार तथा तीन और से ऊँचे हिमशिखरों से घिरी हल्के नीले रंग के इस अण्डाकार कुंड को देखने का सौभाग्य तो वास्तव में साहसी यात्री को ही मिल सकता है। कुंड के किनारे एक छोटा सा मन्दिर स्थित है। इसमें प्राचीन काल की तलवार, पुराने समय के बर्तन व सिक्के रखे हैं। हिमशिखरों के क्षेत्र में बिखरी इस रूपराशि को घंटों तक निहारते रहने में भी मन तृप्त नहीं होता। ऐसा मनोहारी है नन्दीकुंड।

त्रियुगीनारायण
यह रुद्रप्रयाग से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ गंगोत्री पैदल मार्ग पर स्थित है। पुल पार कर गणपति की मस्तकविहीन मूर्ति के दर्शन होते है। यह शीत प्रदेश हैं। यहाँ वन-सम्पदा अत्ति धनी है। यह पावन तीर्थ केदारघाटी में सागरतल से 6000 फीट की ऊँचाई पर अवस्थित है। धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं जनश्रुति यह है कि भगवान शिव और हिमालय पुत्री पार्वती का विवाह संस्कार इसी त्रियुगीनारायण क्षेत्र में हुआ था। मन्दिर के सामने एक चतुष्कोण कुण्ड है, जिसमें तीन युगों से अग्नि जल रही है।
गुप्तकाशी
हरिद्वार से 207 किलोमीटर मोटर मार्ग की दूरी पर गुप्तकाशी, मन्दाकिनी के बांयें तट पर 4352 फीट ऊँचाई पर स्थित एक सुन्दर पुरी है, जो ऊखीमठ के ठीक सामने नदी पार कर है। अगस्त्यमुनि के बाद यह सबसे महत्त्वपूर्ण तीर्थ है। यहाँ से एक मार्ग मध्यमहेश्वर की ओर तथा एक रास्ता ऊखीमठ को भी जाता है। चौखम्भा तथा दूसरी उन्नत श्रृंगों का दृश्य मन को मोहित करता है। इसे काशी के समान पुण्य भूमि माना गया है।

देवताओं ने की थी गुप्त तपस्या
यह भी कहा गया है कि यहाँ पर देवताओं ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए गुप्त रूप से तपस्या की थी। एक दूसरी कथा इस प्रकार है कि अपने कुल का नाश करने वाले पाण्डवों को जब शिव ने दर्शन नहीं देना चाहा तो ये गुप्तकाशी में गुप्त हो गये। यहाँ का प्रमुख विश्वनाथ मन्दिर है, इसमें काशी विश्वनाथ की लिंगमूर्ति है। मन्दिर के सामने मणिकर्णिका कुण्ड है, जिसमें गिरने वाली दो जल धाराओं के जल को स्थानीय निवासी गंगा-यमुना की संज्ञा देते हैं।
ऊखीमठ
पार्श्व में दो शीतल जल के झरने एवं एक कुण्ड भी विद्यमान है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस क्षेत्र में 360 मन्दिर ध्वंसावस्था में है। यहाँ का प्राकृतिक स्वरूप एवं वातावरण आदि देखने पर ऐसा अनुमान होता है कि किसी काल में यह लक्ष्मीनारायण की लीला भूमि रही होगी, तभी इस क्षेत्र को नारायण कोटि कहा जाता है।
कालीमठ
श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग में गुप्तकाशी से कालीमठ के लिए मोटर मार्ग है। यह यात्रा मात्र छ: किलोमीटर दूरी की है। कालीमठ, चौखम्भा क्षेत्र के खाम और मणनी के मध्य मंदाकिनी और सरस्वती नदियों की पीठ में सुशोभित क्षेत्र है। इस सिद्धपीठ में महाकाली, सरस्वती, लक्ष्मी के अति प्राचीन मन्दिरों के अतिरिक्त गौरी शंकर कालीश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव, भैरवनाथ, अघोरकाली के मन्दिर हैं और न बुझने वाला एक अग्निधुना है। इसी प्रांगण में गौरीशंकर की दुर्लभ मूर्ति व एक शिलालेख भी है। गौरीशंकर की मूर्ति के सम्बन्ध में राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि- शोभा और सौन्दर्य में बेजोड़ इसकी कोमल बंकिम रेखाओं में वही सौन्दर्य भरा है जो कि अजन्ता के चित्रों में दिखायी पड़ती है। पत्थर पर ऐसा सुन्दर उत्कीर्णाकन करना सम्भव हो सकता है, इस पर विश्वास नहीं होता।

यहां मां काली की मूर्ति की बजाय है कुंडी
कालीमठ मन्दिर में माँ काली की मूर्ति नहीं अपितु एक कुंडी है, जिसके ऊपर चाँदी की चौकोर शिला रखी रहती है। यहाँ नवरात्रों में पूजा का विशेष आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर शक्ति के उपासक देश के विभिन्न स्थानों से आकर माँ भगवती की कृपा पाने के लिए अनुष्ठान, पूजा और संकल्प करते हैं। माँ काली की कुंडी के चारों ओर वेद पाठी ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, और अन्य लोग निरन्तर माँ दुर्गा का पाठ करते रहते हैं।
ये है किंवदंती
किंवदन्ती है कि राजा भोज नवरात्रों के अवसर पर काली शिला और काली मठ में सैकड़ों वेदपाठी ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। उत्तराखण्ड के विद्वानों के कथनानुसार महाकवि कालीदास इस सिद्धपीठ मन्दिर के पुजारी थे और उनका बचपन का नाम ‘बादरु’ था। किसी नर्तकी से प्रेम हो जाने के कारण उन्हें जातिच्युत कर दिया गया था। जातिच्युत होने पर उन्होंने सिद्धपीठ को त्याग दिया और उज्जयिनी विक्रमादित्य के यहाँ चले गये। यह अकेला सिद्धपीठ क्षेत्र है, जहाँ नवदुर्गा के रूप और स्वरूप के दर्शन होते हैं।
फाटा
यह हरिद्वार से 216 किलोमीटर तथा गुप्तकाशी से 14 किलोमीटर केदारनाथ मार्ग पर पड़ता है। यहाँ की ऊँचाई 5250 फीट है। यहाँ महिषमर्दिनी का मन्दिर है। मूर्ति मनमोहक एवं दर्शनीय है। प्रकृति की अनुपम भेंट वृक्ष, वनस्पतियाँ य वेगवती नदियाँ यात्रियों एवं पर्यटकों को इस क्षेत्र में बार-बार आने का निमन्त्रण देती रहती है।

देवरिया ताल
इस ताल तक पहुँचने के लिए हरिद्वार से श्रीनगर होकर रुद्रप्रयाग पहुँचना पड़ता है। रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ पहुँचकर 13 किलोमीटर उत्तर-पूर्व की ओर पैदल चलने पर इस ताल के भव्य दर्शन होते हैं। यह गढ़वाल का सबसे मनोरम और आकर्षक ताल है। समुद्रतल से 8000 फीट की ऊंचाई पर, पहाड़ की चोटी पर यह ताल तीन किलोमीटर लम्बाई में फैला है। इस ताल में चौखम्भा, नीलकंठ आदि हिमाच्छादित पर्वतों का श्वेत प्रतिविम्ब तथा वृक्षों की हरित छाया सदैव दृष्टिगोचर होती है, जिसके कारण ताल की गहराई का अनुमान लगाना कठिन है। ताल के चारों ओर सुन्दर वृक्षों की छाया और दूर तक फैला हुआ सुन्दर मैंदान इसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा देता है।
केदारनाथ पशु विहार
यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। यह हरिद्वार से लगभग 226 किलोमीटर की दूरी पर ऊखीमठ तहसील के अन्तर्गत है। इस विहार का क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जाने के लिए अनुकूल समय अप्रैल से जून एवं सितम्बर से नवम्बर के बीच का है। इस विहार में मस्क डियर, पैन्थर, काला एवं भूरा हिमालयन भालू, स्नोलैपर्ड, सांभर, भरल तथा मोनाल इत्यादि जंगली पशु पक्षी पाये जाते हैं।

गौरीकुण्ड
केदारनाथ से पहले पड़ने वाला एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीर्थ एवं विश्राम स्थल है। इसकी ऊँचाई 6500 फीट है। यहाँ गरम और ठण्डे पानी के दो कुण्ड हैं। यहाँ गौरी मन्दिर है, जनश्रुति है कि इसी स्थान पर पार्वती ने महादेव को पाने के लिए तपस्या की थी। मन्दिर में गौरी और पार्वती की अष्ट धातु की मूर्तियाँ हैं। दूसरा मन्दिर राधाकृष्णन का है।
तुंगनाथ
ऊखीमठ मोटर मार्ग पर चोपता स्थल तक 32 किलोमीटर यात्रा मोटर मार्ग द्वारा निश्चित
कर शेष तीन किलोमीटर की पैदल चढ़ाई पार कर 12144 फीट ऊँचाई पर तुंगनाथ मन्दिर में पहुँचा जाता है। यह विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर बना प्राचीन मंदिर है। इस मन्दिर में शिव भगवान लिंग के रूप में विराजमान हैं। यह तृतीय केदार के रूप में प्रतिष्ठित है।

यहाँ भगवान शिव की भुजाओं के रूप में पूजा की जाती है। मन्दिर से 650 फीट की ऊँचाई पर चन्दशिला चोटी है, जहाँ तीर्थ यात्री पितृशिला स्फटिकलिंग आदि के दर्शनार्थ जाते हैं। यहाँ से पंचचूली, नन्दादेवी, द्रोणगिरी, नीलकंठ आदि हिमाच्छादित चोटियों के दर्शन के साथ-साथ गढ़वाल व मैंदानी भाग मुरादाबाद तक दिखायी देता है।
मक्कूमठ
शोतकाल में भगवान तुंगनाथ की पूजा मक्कूमत में की जाती है। कपाट खुलने के अवसर पर केदारनाथ की डोली को भांति तुंगनाथ कोडोली मक्कूमठस तुगनाथ के लिए प्रस्थान करती है तथा कपाट बन्द होने पर तुंगनाथ से मक्कूमठ आती है। यह तुंगनाथ का गद्दी स्थल है।
कार्तिकेय मन्दिर
पोखरी रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग पर कनकचौरीसे तीन किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद क्राँच पर्वत पर 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस सिद्धपीठ के दर्शन होते हैं। यहाँ पहुँचकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह पर्वत आकाश छू रहा हो । प्राचीन काल में इस भूमि पर तपस्वी साधु अपनी तपस्या में लीन रहते थे। स्वामी कीर्तिकेय जो कि भगवान शंकर के औरस पुत्र माने जाते हैं। कहते हैं जब इस देवभूमि उत्तराखण्ड में देवासुर संग्राम हुआ था तो कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया था। इस रूप में स्वामी कार्तिकेय को देव सेनापति के रूप में भी पूजा जाता है। कार्तिकेय स्वामी मन्दिर के अन्दर एक स्फुटिक है, जिसका आधार डेढ़ मीटर लम्बा है जो कि दो पत्थरों को काटकर बनाया गया है। स्वामी कार्तिकेय की मूर्ति के अतिरिक्त भैरव का मंदिर व ऐड़ी-अछारी के भी यहाँ छोटे-छोटेॉ मंदिर समूह हैं, जो कि श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
पढ़ने को क्लिक करेंः उत्तराखंड का सबसे विशाल मंदिर केदारनाथ, शिलाखंडों को जोड़कर किया गया निर्मित

लेखक का परिचय
लेखक देवकी नंदन पांडे जाने माने इतिहासकार हैं। वह देहरादून में टैगोर कालोनी में रहते हैं। उनकी इतिहास से संबंधित जानकारी की करीब 17 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। मूल रूप से कुमाऊं के निवासी पांडे लंबे समय से देहरादून में रह रहे हैं।